स्वामी ओमानन्द सरस्वती का जीवन-चरित/षष्ठ अध्याय
(आचार्य भगवानदेव)
(१९१०-२००३) का
जीवन चरित
| षष्ठ अध्याय |
विदेश यात्रा
सितम्बर २७ से ४ अक्तूबर ई० तक दोशाम्बे (सोवियत रूस) में यूनेस्को (UNESCO) के सहयोग से कुषाण काल के संबन्ध में पुरातत्त्व इतिहास और कलाविषयक एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन (International Conference on the Archaeology, Hisotory and Arts of Central Asia in the Kushan Period) हो रहा था । इस सम्मेलन के लिये डॉ० लोकेशचन्द्र, अध्यक्ष, सरस्वती विहार, दिल्ली को निमन्त्रण मिला । एक दिन श्री आचार्य जी उनसे मिलने उनके हौजखास स्थित निवास पर गये थे । उन्होंने आचार्य जे से कहा कि मैं रूस जा रहा हूं । वहां विश्व इतिहास सम्मेलन में मैं मथुरा से प्राप्त एक कुषाण कालीन शिलालेख पर अपना शोध-पत्र प्रस्तुत करूंगा परन्तु मेरे सामने एक कठिनाई है और वह यह है कि उस शिलालेख पर एक चिन्ह है जिसका पता नहीं चल रहा कि यह किसका है या किस उद्देश्य से अंकित किया गया है । डॉ. साहब ने वह चिन्ह बनकर दिखाया तो आचार्य जी ने कहा कि यह चिन्ह तो कुषाण वंश के राजा वासुदेव का है जो उसके सिक्कों पर भी मिलता है । डॉ. साहब ने प्रमाण जानने की उत्कण्ठा प्रकट की तो आचार्य जी ने कहा - यदि आप प्रमाण देखना चाहते हैं तो हमारे यहां पुरातत्त्व संग्रहालय में पधारियेगा, आपको प्रमाण भी मिल जायेगा । तदनुसार वे ३० अगस्त १९६८ ई० को गुरुकुल झज्जर पधारे और उन्होंने विशेषकर कुषाणकालीन पुरातत्त्वीय सामग्री को विशेष रुचि से देखा । गुरुकुल झज्जर संग्रहालय में संगृहीत कुषाण राजाओं के लगभग पाँच हजार सिक्के देखकर डॉ. लोकेशचन्द्र जी ने बहुत आश्चर्य प्रकट किया और पूछा आपने यह अद्भुत संग्रह कहां से और कैसे एकत्रित किया ? साथ ही उन्होंने जब यहां कुषाण वंश के तीन प्रसिद्ध राजा कनिष्क, हुविष्क और वासुदेव प्रथम व द्वितीय तथा कनिष्क तृतीय के मुद्रा-सांचे (coin moulds) देखे तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा । उन्होंने कहा - "आचार्य जी, आपके पास तो कुषाण-वंश की ऐसी सामग्री है जो संसार भर में कहीं नहीं मिलेगी ।"
श्री डॉ० लोकेशचन्द्र जी ने दिल्ली लौटकर उक्त सम्मेलन के प्रबन्धकों को पत्र लिखा - "आचार्य जी के पास बहुत ही दुर्लभ, नई और महत्त्वपूर्ण सामग्री है । यदि आप उन्हें नहीं बुलाते तो आपका यह सम्मेलन अधूरा रह जायेगा ।" यहाँ यह लिखना उचित होगा कि दुर्भाग्य से अपने देश में किसी भी नये महत्त्वपूर्ण कार्य को उतना महत्त्व नहीं दिया जाता जितना कि दिया जाना चाहिये । यही कारण है कि भारत में बहुत कम व्यक्ति किसी नये कार्य को प्रारम्भ करने का साहस कर पाते हैं किन्तु उन्नत देशों में इससे कुछ दूसरी ही स्थिति है । वहां का शासन और समाज दोनों ही किसी भी ऐसे कार्य को पूर्ण सहयोग देकर प्रोत्साहन देते हैं जिससे राष्ट्र का गौरव बढ़ता हो । वे ऐसे कार्य के करने वाले का भी पूरा सम्मान करते हैं । उनकी यह प्रवृत्ति अपने ही कुछ गिने-चुने व्यक्तियों तक सीमित हो, ऐसा भी नहीं है । प्रत्युत दूसरे देश में भी यदि वे ऐसे किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसका भी बहुत आदर करते हैं । इसलिये जब डॉ लोकेशचन्द्र जी के पत्र से उनको आचार्य जी के सम्बंध में पता चला कि इन्होंने कुषाणों से सम्बद्ध बहुत महत्त्वपूर्ण पुरातत्त्वीय सामग्री एकत्रित की है तो उन्होंने वहीं सोवियत रूस से तार व पत्र भेजा - "आचार्य जी ! आप कुषाण इतिहास पर आयोजित इस सम्मेलन में अवश्य पहुंचिये और अपने अनुसंधान से लाभान्वित कीजिये । आपका आने-जाने का वायुयान (हवाई जहाज) का किराया भी हम ही देंगे ।" यह निमन्त्रण-पत्र २७ सितंबर १९६८ ई० को मिला । सम्मेलन २७ सितंबर से प्रारम्भ होना था । पारपत्र तथा विदेशी मुद्रा आदि की औपचारिकताओं के लिये यह समय अत्यल्प था किन्तु कई सहयोगियों के कारण वह सब यथासमय पूरा हो गया ।
२५ सितंबर १९६८ ई० को प्रातः श्री आचार्य जी व डॉ. लोकेशचन्द्र जी ने पालम हवाई अड्डे से दोशांबे (रूस) के लिये प्रस्थान किया । उसी दिन १२ बजे ये अफगानिस्तान के काबुल हवाई अड्डे पर उतरे । वहां एक दिन मित्रोपोल नामक होटल में ठहरे । यहां ये कई हिन्दुओं से भी मिले और एक हिन्दू मन्दिर में भी गये । वहां पता चला कि काबुल में लगभग बीस-पच्चीस हजार हिन्दू बसते हैं । वे अधिकांशतः कपड़े का व्यापार करते हैं । उनकी आर्थिक हालत अच्छी है किन्तु समाज में उनकी स्थिति दयनीय है । बहुधा हिन्दू कन्याओं से वहां बलात् विवाह करने की घटनायें भी होती रहती हैं । अफगानिस्तान में बहुत वर्ष पहले पीर रत्ननाथ नामक एक साधु गया । उसने हिन्दुओं को उत्साहित किया । उनमें प्रचार कार्य भी किया । उसी के कारण वहां आज भी हिन्दू हैं । इस साधु की काबुल में अनेक जगह पर समाधियां बना रखी हैं और हिन्दू लोग वहां पूजा भी करते हैं । काबुल हवाई अड्डे पर अनेक वायुयानों पर 'आर्याना एयरवेज' लिखा था । एक होटल का नाम भी 'आर्याना होटल' था जहां रूस से वापिस लौटते हुए आचार्य जी ठहरे । क्योंकि अफगानिस्तान और ईरान के लोग अपने आपको आर्यों का वंशज मानते हैं ।

अगले दिन काबुल से रूसी वायुयान द्वारा चलकर ताशकन्द होते हुये आप दोशाम्बे पहुंचे । यहां २७ सितम्बर से ४ अक्तूबर तक उपर्युक्त सम्मेलन चला । १ अक्तूबर को श्री आचार्य जी ने सम्मेलन में अपना शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत किया । विषय था "The Last Struggle of the Kushannas in India" (कुषाणों का भारत में अन्तिम संघर्ष) ।" क्योंकि आचार्य जी का शोधपत्र पुरातत्त्वीय गवेषणाओं पर आधारित और प्रमाणसम्मत था अतः उसका बहुत अच्छा प्रभाव रहा । देश विदेश के अनेक प्रख्यात विद्वानों ने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की । अनेक ने भारत आकर आचार्य जी द्वारा संस्थापित संग्रहालय देखने की इच्छा प्रकट की । विदेशी विद्वानों के लिये यह बड़े आश्चर्य की बात थी कि एक महात्मा या साधु इस तरह की गम्भीर खोज कर रहा है । क्योंकि बाह्य देशों में हमारे देश के साधु-संन्यासियों की जो प्रतिमा है वह या तो बहुत विकृत है या मात्र आध्यात्मिकता तक ही सीमित है । पहली बार वे एक श्वेत वस्त्रधारी साधु को इतिहास और पुरातत्त्वीय प्रमाणों के आधार पर कुषाण इतिहास सरीखे जटिल और मतभेदपूर्ण विषय पर बोलता हुआ सुन रहे थे । यह वास्तव में उनके लिये ही नहीं, भारत से जाने वाले विद्वानों के लिए भी आश्चर्य की बात थी । यद्यपि भारत से जाने वाले इतिहास के सभी विद्वानों ने पहले से ही आचार्य जी का नाम तो सुन रखा था और अधिकांश उनके कार्य से भी परिचित थे, परन्तु उनमें से दो-तीन को छोड़कर आपको देखा किसी ने नहीं था ।
स्मरण रहे श्री आचार्य जी रूस भी अपनी उसी वेशभूषा में गये जिसमें वे यहां रहते हैं - एक कटिवस्त्र, ऊपर एक चद्दर और सर्वथा नंगे पैर, सिर पर लम्बी चोटी । भोजन भी आपका विदेश में वही रहता है । नमक व मीठे रहित सर्वथा शाकाहारी । दूध और घी भी आप वहां भी गाय का ही प्रयोग करते रहे । दिनचर्या भी आपकी यहां जैसी ही रही । प्रातः नित्य संध्या व हवन करते रहे । इस सबको देखकर आप वहां आकर्षण का केन्द्र बने रहे । वहाँ अन्यों की अपेक्षा आदर भी आपको सर्वाधिक मिलता रहा । जिस समय आपको निमन्त्रण मिला तो सम्मेलन के आयोजकों ने आपको अपने रहने और आवास का व्ययभार स्वयं वहन करने के लिये लिखा था किन्तु जब आप वहां होटल में किराया आदि देने लगे तो उन्होंने लेने से इन्कार किया और कहा आपका सम्पूर्ण व्यय हमारा शासन वहन करेगा । यह आचार्य जी के प्रभाव का ही फल था । वहां रहकर आपने रूस के दो प्रदेश ताजकिस्तान और उजबेकिस्तान की संस्कृति और सभ्यता का विशेष रूप से अध्ययन किया जिसको आपने अपने यात्रा विवरण "रूस में पन्द्रह दिन" में प्रकाशित किया है । इसमें आपने अपनी रूस-यात्रा का पूरा वृत्तान्त लिखा है । १० अक्तूबर १९६८ को आप रूस से वापिस लौट आये ।
रूस से वापिस लौटने पर १५ अक्तूबर को नरेला में श्री आचार्य जी व डॉ लोकेशचन्द्र जी के सम्मान में एक विशाल स्वागत समारोह का आयोजन हुआ । इसमें बोलते हुये श्री विद्याचरण शुक्ल तत्कालीन गृहराज्य मंत्री भारत सरकार ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि श्री आचार्य जी अपनी भारतीय और वह भी साधु की वेशभूषा में ही रूस में रहे । वास्तव में यह बात कहने और सुनने में बहुत सामान्य और हल्की प्रतीत होती है परन्तु इसका प्रभाव कितना गहरा होता है यह विचारने की बात है । यदि हम अपनी वेशभूषा में बाहर जाते हैं तो हमें और हमारे माध्यम से देश को सम्मान मिलता है । जिस व्यक्ति या देश को अपनी राष्ट्रीयता, अपनी वेशभूषा और अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं, वह प्रगति भी नहीं कर सकेगा ।
संन्यास-दीक्षा
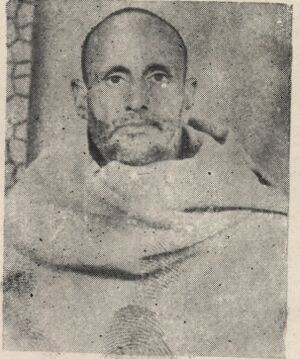
आचार्य जी महाराज का जीवन यौवनावस्था से एक सधे हुये संन्यासी का जीवन रहा है । अपने सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य जीवन में वे एक कठोर तपस्वी, श्रद्धालु साधक, आध्यात्मिकता से ओतप्रोत व्रती संन्यासी के रूप में रहे हैं । सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन्होंने अपने जीवन में कभी दिखावा नहीं किया । आडम्बर इनके जीवन में कभी आ ही नहीं पाया । हमने भी अपने छोटे से जीवन में अनेक साधु संन्यासी देखे हैं परन्तु आचार्य जी जैसी संन्यस्तवृत्ति का उनमें कोई भी देखने को नहीं मिला । जीवन के उषाकाल में ही इन्होंने घर-बार छोड़ा, अथाह सम्पत्ति छोड़ी, सगे संबन्धी छोड़े और मां बाप को छोड़ा । एक बार यह सब छोड़ा तो फिर छोड़ ही दिया । कभी उधर मुंह करके भी नहीं देखा यह कितना कठोर व्रत है । इसको अच्छी प्रकार केवल वे ही व्यक्ति समझ सकते हैं जिन्होंने जीवन में कोई व्रत रखने या त्याग की डगर पर कदम रखने का प्रयास किया है । अनेक साधु-संन्यासी या वानप्रस्थी ऐसे भी हैं जो मोह को नहीं छोड़ पाते और घर जाकर अपने परिवारिकजनों से मिलते रहते हैं, भले ही उन्हें चोरी-छिपे मिलना पड़े । अनेक ऐसे हैं जो लोकलाज के कारण स्वयं तो घर नहीं जाते किन्तु घरवालों को अपने पास बुला लेते हैं और समाज का पैसा उन्हें देते रहते हैं । अनेक ऐसे हैं जो "पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा माया परित्यक्ता" कहकर भी इनमें लिप्त रहते हैं । मैं समझता हूँ पुत्र और वित्त की ऐषणा-इच्छा का त्याग तो कई लोग कर सकते हैं किन्तु लोकैषणा छोड़ना बड़ा कठिन कार्य है । पाठकगण ! आपने भी अनेक ऐसे संन्यासी देखे होंगे जो पद और नाम के लोभ में अपने काषाय वस्त्रों की गरिमा को ताक पर रख राजनैतिक नेताओं के तलवे चाटते फिरते हैं । किसी राजनैतिक नेता से उसकी उच्च मानवीयता और ईमानदारी के कारण किसी का संबन्ध होना अलग बात है किन्तु मात्र किसी पदप्राप्ति के लिये इन लोगों का पिछलग्गू बनना तो संन्यास धर्म पर कलंक लगाना है । मैं समझता हूं ऐसे संन्यासियों के कारण ही फिर साधुओं के प्रति लोगों की अश्रद्धा हो जाती है । ऐसे साधुओं से तो गृहस्थी अच्छे जो कम से कम अपने बच्चों व परिवार के प्रति तो उत्तरदाई और ईमानदार हैं किन्तु ऐसे संन्यासियों का क्या जो स्वयं अपनी आत्मा के प्रति भी ईमानदार नहीं ।

हमारे चरित्रनायक पूज्य आचार्य स्वामी ओमानन्द सरस्वती को ऐसी तुच्छ ऐषणायें जीवन कें कभी छू भी नहीं पाईं हैं । इनकी चिरन्तन तपस्या में यह सब इच्छायें भस्मसात् हो गईं हैं । किसी पारिवारिक या सम्बंधी की सहायता करना तो बहुत दूर रहा, इन्होंने तो कभी अपने लिये भी संस्था या समाज का पैसा व्यय नहीं किया । मुझे अनेक वर्षों तक इनके निकट सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । जितने लगाव रहित निश्छल और निस्पृह ये हैं उतना शायद ही दूसरा कोई होगा । कठोर तप, त्याग से परिपूर्ण दुनियादारी से सर्वथा दूर आचार्य जी महाराज प्रारम्भ से ही संन्यासी हैं किन्तु सन् १९७० ई० में इन्होंने विधिवत् दीक्षा लेकर ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यासाश्रम में प्रवेश किया । इस दीक्षा को भी इन्होंने अपने स्वभावानुसार अत्यन्त गुप्त रखा । किसी प्रकार का कोई प्रचार नहीं, कोई दिखावा नहीं । शास्त्रविधिसम्मत विशुद्ध सात्विक तरीके से इनकी दीक्षा-विधि सम्पन्न हुई ।
अप्रैल १९७० में आचार्य जी गुरुकुल घरौंडा के उत्सव पर गये । ब्रह्मचारी विरजान्द दैवकरणि, ब्र० धर्मवीर (महाराष्ट्र) और ब्र० विक्रम (उड़ीसा) इनके साथ थे । आचार्य जी ने घरौंडा से ही संस्कारविधि पढ़ना प्रारम्भ कर दिया । यहां से आप आर्यसमाज बटाला के उत्सव पर पहुंचे । वहां आचार्य जी के दो व्याख्यान हुये किन्तु आपने भोजन वहां भी नहीं किया । वहां इन्होंने ब्र० धर्मवीर को एक ओर ले जाकर अपने कुछ कपड़े दिये और समझा दिया कि जाओ दीनानगर जाकर स्वामी सर्वानन्द जी महाराज से प्रार्थना करो कि मुझे संन्यास दीक्षा देने की तैयारी करें परन्तु उनको यह भी आदेश दिया कि इस बात का पता ब्र० विरजानन्द की आदि को भी नहीं चलना चाहिये । जब तीन दिन से आचार्य जी ने भोजन नहीं किया तो विरजानन्द जी ने इनसे भोजन के लिये आग्रह किया किन्तु ये टाल गये और निराहार ही रहे । दयानन्दमठ दीनानगर में भी ४ अप्रैल १९७० को प्रातः ३ बजे ही पहुँचे जबकि उसी दिन प्रातः दीक्षा लेनी थी । वहां जाकर भी ब्र० विरजानन्द जी आदि को तब तक पता नहीं चल पाया जब तक कि ये यज्ञवेदी पर नहीं पहुंचे । वहां पहुंचने पर ही ज्ञात हो सका कि पिछले तीन-चार दिन से आचार्य जी महाराज जो कुछ कर रहे थे वह सब इस दीक्षा की सज्जा हेतु ही कर रहे थे किन्तु महान् हैं आचार्यप्रवर ! अपने जीवन की इतनी बड़ी घटना को भी इन्होंने कितने सहज भाव से लिया । कहां तो वे लोग जो संन्यास प्रवेश को भी आडम्बरपूर्ण बनाकर उसको प्रचार का माध्यम बनाते हैं और कहां यह दीक्षा ?

आचार्य जी महाराज ने अपना दीक्षागुरु भी एक ऐसे महात्मा को ही चुना जो सच्चे अर्थों में संन्यासी है । सब प्रकार की ऐषणाओं और महत्त्वाकांक्षाओं से सर्वथा दूर रहकर भगवद् भजन और गरीबजनों की सेवा ही जिनका परम व्रत है । हजारों रुपयों की महंगी से महंगी औषधियां भी जो गरीबों में मुफ्त बांटते रहते हैं । केवल आर्यसमाजी ही नहीं, अपितु सनातनी सिक्ख और मुसलमान भी जिनको अपना श्रद्धेय मानते हैं । ऐसे पूज्य स्वामी सर्वानन्द जी महाराज को श्री आचार्य जी महाराज ने अपना दीक्षागुरु बनाया । उनके प्रति आचार्य जी की प्रारम्भ से ही अत्यधिक श्रद्धा रही है ।
स्वामी जी ने जब आचार्य जी को संन्यासाश्रम में दीक्षित किया तो दयानन्दमठ दीनानगर की यज्ञवेदी पर प्रतिदिन की भांति लगभग पचास व्यक्ति वहां उपस्थित थे । सम्पूर्ण विधि-अनुसार दीक्षा देकर स्वामी जी महाराज ने आचार्य जी का परिवर्तित नाम घोषित किया । और वे अब आचार्य भगवानदेव से स्वामी ओमानन्द सरस्वती हो गये । स्वामी जी ने अपने दीक्षागुरु के चरण छुये । इस तरह एक तेजस्वी ब्रह्मचारी ने जिसने जीवनभर अन्याय और अत्याचारों से टक्कर ली, संन्यासाश्रम में प्रवेश किया । इनका यह कार्य भी उतना ही आदर्श था जितने कि जीवन के पहले कार्य ।
संन्यासग्रहण कर दयानन्दमठ दीनानगर से चलकर आप कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय होते हुये कन्या गुरुकुल नरेला आये । यहाँ सूबेदार धीरजसिंह जी व वैद्य कर्मवीर जी आदि व्यवस्थापकों तथा ब्रहमचारियों को आचार्य जी को काषाय वस्त्रों में देखकर कुतुहल होना स्वाभाविक था । कुछ तो रोने भी लगे कि स्वामी जी महाराज अब हमें छोड़कर चले जायेंगे । उन्होंने स्वामी जी से प्रार्थना भी की कि आप कृपया इस कार्यक्षेत्र को छोडिये मत । आप तो पहले से ही संन्यासी रहे हैं । यहां से आप गुरुकुल झज्जर पधारे । वहां भी ऐसी ही प्रतिक्रिया हुई । वहां ब्रह्मचारियों ने स्वामी जी से बहुत अधिक आग्रह कर अपने साथ उनके चित्र (फोटो) लिवाये । वहां से ७ अप्रैल को स्वामी जी महाराज दयानन्दमठ रोहतक पहुँचे । यहां दो युवा ब्रह्मचारी श्री इन्द्रवेश व अग्निवेश जी राजशाही ढ़ंग से संन्यास दीक्षा ग्रहण कर रहे थे । यहां हजारों आर्यसमाजी उपस्थित थे । उन्होंने भी अब आचार्य जी को संन्यासी वेश में देखा ।
जापान, फार्मोसा तथा थाईलैंड यात्रा
२८ अगस्त १९७० ई० को जापान से 'कोयासान यूनिवर्सिटी' के प्रोफेसर और 'बुद्धिस्ट म्यूजियम रिहोकान' के अध्यक्ष श्री डा० चिक्योयामा मोतो ने स्वामी ओमानन्द जी महाराज को हरयाणा प्रान्तीय पुरातत्त्व संग्रहालय गुरुकुल झज्जर के अध्यक्ष के नाते निमन्त्रण भेजा - "आशा है आप हमारा निमन्त्रण स्वीकार करेंगे और हमारे म्यूजिमय की बौद्धकला वस्तुओं को देखकर आप सन्तुष्ट होंगे । जापान में आपकी यात्रा आदि का व्यय सब हमारा म्यूजियम उठायेगा ।" यह निमन्त्रण डा० लोकेशचन्द्र जी सहित आप दोनों को मिला था । डा० लोकेशचन्द्र जी वृहत्तर भारत के महान् गवेषक हैं । उनके कन्धों पर राष्ट्रभाषा और लुप्त संस्कृति का रूप निखारने और संवारने का गुरुतर भार है । वे सुदूर पूर्व के एशियाई देशों में भारत के अतीत संबन्धी इतिहास और संस्कृति का अनुसंधान कार्य भी करते हैं । बहुधा राजनीति में भी प्रवेश रखते हैं । अतः वे विदेश के अनेक निमन्त्रण छोड़ देते हैं किन्तु इस बार चूंकि श्री स्वामी जी महाराज को भी साथ जाना था, इसलिये वे भी तैयार हो गये ।
स्वामी जी का जीवन भी व्यस्तताओं से परिपूर्ण रहता है । जापान से निमन्त्रण आने से पूर्व ही ये आर्यसमाज जम्मू को एक सप्ताह वेदकथा के लिये दे चुके थे । जम्मू जाने से पूर्व ये श्री बाबू जगन्नाथ जी बी.ए.एल.एल.बी. को विदेशी मुद्रा और वीजा आदि का कार्य सौंप गये । २ सितंबर को उन्होंने स्वामी जी को ट्रंककाल कर जम्मू में सूचित किया कि आपको स्वयं आना होगा जिससे कार्य समय पर हो सके । स्वामी जी ५ सितंबर को वहां से आकर दिल्ली पहुंच गये । आप दोनों इतनी विदेशी मुद्रा चाहते थे जिससे एक मास विदेश में रहा जा सके । क्योंकि जापान से वापिस लौटते हुये आप दोनों थाईलैंड, बाली और जावा आदि उन कई द्वीपों में जाना चाहते थे जहाँ की धरती पर आज भी भारतीय संस्कृति पलती है और हिन्दुत्व की रक्षा हो रही है । इन द्वीपों से ये कुछ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व की सामग्री भी लाना चाहते थे किन्तु समस्या यह थी कि प्रयास करने पर १५ दिन की भी विदेशी मुद्रा नहीं मिल पा रही थी ।
अन्ततोगत्वा श्री प्रो० शेरसिंह, श्री विद्याचरण शुक्ल, श्री रघुवीरसिंह शास्त्री तथा बाबू जगन्नाथ जी के प्रयत्न से १५ दिन तक विदेश में रहने योग्य विदेशी मुद्रा मिल गई । इसे एक विडम्बना ही कहना चाहिये कि देश के लिये अमूल्य निधि बटोरने के लिये जाने वालों के साथ भी विदेशी मुद्रा के मामले में वैसा ही व्यवहार किया जाता है जैसा कि एक सामान्य पर्यटक के साथ होता है ।
११ सितंबर को आप दोनों पालम हवाई अड्डे से एक डच वायुयान द्वारा जापान के लिये उड़े । बैंकाक (थाई देश) और मनीला होते हुये जापान की राजधानी टोकियो पहुंच गये । टोकियो से ओसाका पहुँचे और वहां एक्सपो ७० विश्वमेला देखने गये । जापान की व्यापारिक राजधानी ओसाका में आयोजित इस विश्व मेले से जापान को जहां कला, उद्योग, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में बहुत कुछ सीखने और सिखाने का अवसर मिला, वहां दूसरी ओर उसे करोड़ों येन का विशुद्ध लाभ भी हुआ । विदेशी मुद्रा अर्जित करने का भी अवसर उसको मिला । ओसाका शहर जापान में टोकियो के बाद दूसरे नम्बर पर माना जाता है । इसकी सुन्दर चौड़ी सड़कें लाजवाब हैं । स्वच्छता यहां का गहना है । व्यापारिक केन्द्र होने के नाते यह शहर जापान के दूसरे बड़े नगरों से परिवहन एवं यातायात से भलीभांति जुड़ा है । यहां के पुराने ऐतिहासिक स्थानों में सबसे प्राचीन ओसाका दुर्ग है । यह १८५८ ई० में बना था ।
यहां से आप क्योतो गये । वहां अनेक बौद्ध मन्दिरों में भी आप गये । यहां के "सान्जूशन गैंदो" मन्दिर में तो ७००१ मूर्तियां हैं । ये मूर्तियां यद्यपि लकड़ी की हैं किन्तु इस पर स्वर्ण का पानी फेर दिया गया है । यहां स्थापित एक विशालकाय मूर्ति के एकादश (ग्यारह) मुख और एक सहस्र भुजायें दिखाई हैं । यह अवलोकितेश्वर की मूर्ति है । इसके पृष्ठभाग में इन्द्र, अग्नि और वायु आदि हिन्दू देवताओं की मूर्तियां बनी हैं । यह पूरा मन्दिर लकड़ी का बना है । क्योतो के सभी मन्दिरों में अगरबत्ती तथा धूपबत्तियां जल रही थीं । इन मन्दिरों में कई मन्दिर ऐसे हैं जो ७०० वर्ष से १२०० वर्ष पुराने हैं । जापान में इनकी सुरक्षा का बहुत अधिक ध्यान रखा जाता है । अनेक मन्दिर ऐसे भी हैं जिन पर करोड़ों रुपया व्यय किया गया है । प्रायः सभी मन्दिरों पर चीनी वास्तुकला का प्रभाव है । इसका कारण यह है कि बौद्धधर्म भारत से चलकर पहले चीन पहुंचा और वहां से जापान ।

यहां एक विचित्र घटना घटी । १४ सितंबर १९७० ई० को स्वामी जी शौच स्नानादि से निवृत्त हो, होटल के अपने कमरे में हवन करने बैठ गये । यहाँ प्रायः सभी होटलों में अग्नि प्रज्वलित करने का निषेध है । अनेक होटलों में ऐसे यन्त्र भी लगे होते हैं जो आग जलते ही प्रबन्धकों को सूचित कर देते हैं और आग को तुरन्त शांत कर दिया जाता है । अब भी ऐसा ही हुआ । ज्यों ही स्वामी जी ने यज्ञाग्नि प्रज्वलित की, यन्त्र ने सूचना दी कि अमुक कमरे में आग लगी है । बस फिर क्या था । होटल में खतरे का संकेत गूंज गया और वहां ठहरे सभी लोगों में भगडड़ मच गई । सब एक दूसरे से पहले निकल कर प्राण बचाकर भाग जाने की चिन्ता में थे । अनेक व्यक्ति अपना आवश्यक सामान उठाकर भागने लगे । होटल के दुर्घटना द्वार (एमरजेन्सी द्वार) खोल दिये गये । इतनी देर में एक घबराई और हड़बड़ाई हुई होटल की परिचारिका आई । उसने स्वामी जी वाले कमरे का द्वार खोला तथा हवन कुण्ड में जलती यज्ञाग्नि को देखकर बहुत घबरा गई । उसने हाथ तथा शारीरिक चेष्टाओं से इस प्रकार के भाव प्रकट किये मानो यह अग्नि पूरे होटल को स्वाहा कर देगी । स्वामी जी का हवन कुण्ड एक बड़े कटोरे में और कटोरा होटल की एक बड़ी प्लेट में रखा था । अतः न तो कमरे का फर्श खराब होने की कोई बात थी और न ही आग लगने का कोई भय । स्वामी जी ने इस बात को संकेत द्वारा उसे समझाया भी कि यज्ञाग्नि कुण्ड से बाहर नहीं जायेगी किन्तु भाषा के अन्तराल के कारण इन दोनों की स्थिति उस आदमी की सी थी जो कहना तो बहुत कुछ चाहे, पर कह कुछ भी न सके । एक ओर होटल परिचारिका को आग लग जाने का भय कंपित कर रहा था, दूसरी ओर स्वामी जी महाराज अपना स्पष्टीकरण देने के लिये विह्वल थे । आखिर संकेतों द्वारा वह स्वामी जी के भाव समझ गई और शान्त होकर नीचे चली गई । तभी डा० लोकेशचन्द्र जी अपने दूसरे कमरे से स्नान कर वहां आ पहुंचे और उन्होंने नीचे जाकर होटलवालों को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जिससे उनके मन में अन्यथा भाव न रहे । क्योतो में इन्होंने विश्वविद्यालय भी देखा । इस विश्वविद्यालय के प्रतीक्षा कक्ष में हाथ में पुस्तक व पूर्णघट लिये देवी की एक बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई थी । यहाँ बौद्धधर्म और संस्कृत विभाग में १८० उपस्नातक व स्नातक विद्यार्थी हैं ।
क्योतो से स्वामी जी नारा गये । यहां इन्होंने ७४५ ई० में स्थापित एक प्राचीन मन्दिर देखा । यहां भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा है । इस मूर्ति की लम्बाई ५३ फुट, चेहरे की लम्बाई १५ फुट, चौड़ाई ९ फुट पांच इंच । इसकी एक-एक आँख ३ फुट ९ इंच की है । कान की लम्बाई ८ फुट ५ इंच, घुटनों की लम्बाई ८ फुट ५ इंच है । घुटनों की मोटाई ७ फुट तथा दोनों घुटनों के बीच का अन्तर ३ फुट ८ इंच है । अंगूठे की लम्बाई ५ फुट ३ इंच है । इसके घुंघराले बालों की लटों की संख्या ९६६ है । इस मूर्ति का कुल भार ५०० मीट्रिक टन है । यह तोजाई मन्दिर तथा नारा शहर इस मूर्ति के कारण संसारभर में प्रसिद्ध है ।
२२ सितंबर को इनके मेजबानों ने इनके लिए प्रैस कान्फ्रेंस का प्रबन्ध किया । जहां प्रेस कान्फ्रेंस हो रही थी वह एक समाचारपत्र का कार्यालय था । उसमें कई जगह संस्कृत मन्त्र लिखे थे । अगले दिन जापानी दैनिक समाचारपत्रों में स्वामी जी व डा० लोकेशचन्द्र जी के चित्रों सहित उनके सुझावों को बड़ी प्रमुखता से छापा ।
जापान के कई विश्वविद्यालयों में आप दोनों के अनेक भाषण हुये । वहां से महत्त्वपूर्ण सामग्री भी प्राप्त की और वहां के संग्रहालयों का अध्ययन किया । डा० लोकेशचन्द्र जी अपनी इस यात्रा में अपने साथ गंगाजल भी ले गये थे । स्वामी जी तथा उन्होंने थाईलैंड के कई मन्दिरों आदि से जब पैसे से प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ व सिक्के खरीदने चाहे तो वहां के लोगों ने इन्कार कर दिया किन्तु जब उन्हें गंगाजली दी गई तो ये वस्तुयें सहज में ही प्राप्त हो गईं । थाईलैंडवासी भारतीयों को देखकर भारी श्रद्धा प्रकट करते हैं और कहते हैं कि भारत जाकर गंगाजल अवश्य भेजना । इसका विस्तृत विवरण 'जापान यात्रा' नामक पुस्तक में विस्तार से दिया है । यहां आप उस मन्दिर में भी गये जहां प्रसिद्ध क्रान्तिकारी सुभाष बाबू के अवशेष रखे हुये हैं ।
जापान से ताईवान (फार्मोसा) गये । फार्मोसा में जिधर देखो लामाओं के रूप में चारों ओर बौद्ध भिक्षु दिखाई पड़ते थे । वहां प्रत्येक व्यक्ति जीवन में भिक्षु अवश्य बनता है । २० वर्ष से पहले कोई भिक्षु नहीं बन सकता । सब भिक्षु सिर मुंडवा कर त्यागमय जीवन व्यतीत करते हैं । फार्मोसा सांस्कृतिक दृष्टि से छोटा भारत है । वहां के लोगों के मन में आज भी भारतीयों के लिये प्रेम और आदर है । इसी कारण उन्होंने आपको भी राजकीय अतिथि के रूप में ठहराया और स्वागत किया । वहां के अनेक संसद्सदस्यों और राजनयज्ञों ने आपको भोजन पर निमन्त्रित किया ।
चार दिन ताईवान में व्यतीत कर और वहां की संस्कृति तथा जनजीवन का अध्ययन कर ४ अक्तूबर को आप थाईलैंड के लिये प्रस्थान कर गये । ताईवान से एक घंटे बात हांगकांग पहुंच गये । यहां लगभग १० हजार भारतीय रहते हैं । दो हिन्दू मन्दिर और एक गुरुद्वारा भी है । यहां चीनी अधिक संख्या में हैं - लगभग तीस लाख । यहां से चीन की सीमा केवल ४५ मील है । ६ घंटे हांगकांग में घूमने के उपरान्त आप थाई देश की राजधानी बैंकाक के लिये चले । वहां आपने अनेक हिन्दू व बौद्ध मन्दिरों की यात्रा की । इस देश में बौद्धों का बहुत अधिक मान है । बौद्धों के अतिरिक्त अन्य भारतीय देवताओं की भी पूजा होती है । थाईलैंड के राजा अपने को विष्णु का अवतार मानते हैं । रामायण का यहां बहुत प्रचलन है । कला में हर जगह रामायण का बोलबाला है ।
यहां महात्मा बुद्ध की एक स्वर्ण-मूर्ति साढे पांच टन की है । जब बर्मा वाले इनकी सब मूर्तियां उठाकर ले गये तब इस भारी मूर्ति पर एक भिक्षु ने चतुराई से सीमेंट पुतवा दिया जिससे यह बच गई । यहां आर्यसमाज मन्दिर भी है जिसकी स्थापना १९५४ में हुई थी । यहां के राष्ट्रीय पुस्तकालय में ५८ हजार ग्रन्थ हस्तलिखित हैं जिनमें से ३६ हजार काले नीले कागज पर हैं । २२ सहस्र ताम्रपत्र पर हैं । इस देश के अनेक स्थानों की स्वामी जी व डा० लोकेशचन्द्र जी ने यात्रा की और वहां के अनेक हस्तलिखित ग्रन्थ आदि प्राप्त कर २६ दिन की यह विदेश यात्रा पूरी कर आप अपनी मातृभूमि वापिस लौट आये ।
आस्ट्रेलिया, सिंगापुर, बाली तथा इंडोनेशिया यात्रा
जापान यात्रा से लौटने के कुछ मास बाद स्वामी जी अपनी तीसरी विदेश यात्रा पर निकले । आस्ट्रेलिया में हो रही 28th International Congress of Orientalists (प्राच्यविदों का २८वां अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन) का स्वामी जी को निमन्त्रण पत्र मिला किन्तु उन्होंने मार्गव्यादि का प्रबन्ध कर सकने में असमर्थता प्रकट की । ऐसी अवस्था में स्वामी जी जैसे व्यक्ति के लिये जो जीवन में एकान्ततः भिखारी हैं या यूं कहना चाहिये कि जो अपने ऊपर निज के लिये मिला पैसा भी व्यय न कर संस्थाओं को दे देते हैं, का जाना असम्भव सा हो गया । दूसरे, स्वामी जी का यह स्वभाव है कि वे समाज से अपने लिये कुछ लेने की अपेक्षा समाज को कुछ देना अच्छा समझते हैं । निरन्तर इसी प्रकार के चिन्तन ने उनके स्वभाव को भी इसी ढ़ांचे में ढाल दिया है । जब कभी ये संस्था या समाज का द्वव्य अपने लिये व्यय होता देखते हैं तो इन्हें बहुत अखरता है और ये दुःखी हो जाते हैं । इसलिये शुभचिन्तकों द्वारा बार-बार कहने पर भी इन्होंने आस्ट्रेलिया सम्मेलन में जाने से स्पष्ट इन्कार कर दिया किन्तु केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय इनके लिये मार्ग व्यय आदि की सब सुविधायें जुटाने के लिये तैयार हो गया । अतः जाने में अब कोई कठिनाई नहीं रही ।
३ जनवरी १९७१ को 'हरयाणा ग्रामीण परिषद् दिल्ली' ने स्वामी जी की विदाई में हरयाणा भवन दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया । ४ जनवरी को इन्होंने आस्ट्रेलिया के लिये प्रस्थान किया । ४ जनवरी को इन्होंने आस्ट्रेलिया के लिये प्रस्थान किया । अगले दिन आप कैनबरा पहुंचे । वहां बर्टन होटल में ठहरने की व्यवस्था थी । इस बार भारतीय प्रतिनिधि मण्डल में डॉ. नुरुल हसन, डॉ. लोकेशचन्द्र और डॉ. शिवराम मूर्ति तथा डॉ. श्रीमती कपिला वात्स्यायन आदि भी थे । इस सम्मेलन में स्वामी जी ने अपना शोध-लेख 'Ancient Seals of Yaudheya Republic' (यौधेयगण की प्राचीन मोहरें) पढ़ा । एक सम्मेलन में चीन को छोड़कर संसार के सभी प्रमुख देशों के विद्वान् भाग ले रहे थे ।
१३ जनवरी १९७१ को आस्ट्रेलिया से चलकर स्वामी जी सिंगापुर पहुंचे । वहां आप आर्यसमाज मंदिर में ठहरे । उस समय वहां आर्यसमाज के मन्त्री श्रीधर त्रिपाठी थे । उन्होंने स्वामी जी को कहा कि अभी कुछ दिन पहले हमने आपको निमन्त्रण भेजा था किन्तु स्वामी जी उस समय आस्ट्रेलिया में थे । यहां तीन-चार दिन स्वामी जी सत्संगों में प्रवचन करते रहे । एक सत्संग में तो ५०० व्यक्ति उपस्थित थे । स्वामी जी का बड़ा प्रभाव हुआ । वहां के लोग कम से कम एक मास रोकने का आग्रह कर रहे थे किन्तु स्वामी जी का पहले से ही कार्यक्रम तय था और इंडोनेशिया जाना था । इनको लौटते हुये आने का वचन दे स्वामी जी इंडोनेशिया पहुंच गये ।
इंडोनेशिया में आपका पूर्व परिचित कोई नहीं था । वहां आप एक गुरुद्वारे में ठहरे । वहां आपने आधा घंटा सत्संग में राम और कृष्ण के संबन्ध में व्याख्यान दिया । वहां सत्संग में पांच छः व्यक्तियों को छोड़कर सब मुन्ने हिन्दू थे । वहां की राजधानी जकार्ता में स्वामी जी ठहरे । वहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं । चीनी व जापानियों के अतिरिक्त पांच छः हजार भारतीय भी हैं । अगले दिन भी स्वामी जी "अनुव्रतः पितुः पुत्रो..." मन्त्र पर एक घण्टा बोले । वहां हिन्दू ज्योतिषाचार्यों की बनाई वेधशाला भी इन्होंने देखी । स्कूल के प्रिंसीपल ने इनके व्याख्यान का अंग्रेजी अनुवाद किया । यहां अनेक पारिवारिक सत्संगों में भी स्वामी जी के उपदेश हुये । जहां कोई भी परिचित नहीं था वहां अब सैंकड़ों परिचित हो गये और स्वामी जी से जकार्ता के लिये अधिक समय देने का आग्रह करने लगे ।
जकार्ता से आप इस देश के दूसरे प्रसिद्ध नगर जोग्यकर्ता पहुंचे । वहां श्री छबीलदास सिन्धी के यहां ठहरे । जिस समय डॉ. सुकर्णो को अपदस्थ किया तो सब भारतीय अपने परिवारों को भारत छोड़ गये थे । सुकर्णो की हिन्दू धर्म और संस्कृति में गहरी रुचि थी । उसकी मां बाली द्वीप की एक हिन्दू देवी थी, जबकि पिता मुसलमान थे । जोग्यकर्ता राज्य की विमान सेवा का नाम "गरुड़" है । यहां के मन्दिरों को देखने से ऐसा लगता है जैसे हम दक्षिण भारतीय मन्दिरों को देख रहे हैं । शिव, ब्रह्मा, विष्णु, गणेश, उमा, महेश्वर, कुबेर, बुद्ध, अवलोकितेश्वर तथा सरस्वती आदि की सभी मूर्तियां यहां विद्यमान हैं । प्राचीन समय में हिन्दू धर्म का बोलबाला था परन्तु मूर्तियों की पूजा नहीं होती थी । अब पूजा होती है । अब भी बाली आदि द्वीपों में लोग मन्त्रपाठ कर भगवद् आराधना करते हैं ।
स्वामी जी यहां से संसार प्रसिद्ध बोरोबुडुर बौद्ध विहार देखने गये । यह अत्यधिक विशाल है । कई मंजिला है । भगवान बुद्ध की यहां हजारों मूर्तियां हैं ।
यहां से चलकर २४ जनवरी १९७१ को स्वामी जी बाली द्वीप पहुँचे । स्वामी जी ने यहां एक मन्दिर में २५ रुपये दान दिये । यहां सभ्य व्यक्ति को आर्य कहा जाता है । यहां के मन्दिरों में सर्वत्र रामायण और महाभारत के कथानकों के आधार पर मूर्तियां अंकित हैं । डॉ. सुकर्णो ने यहां के हिन्दुओं को कभी मुसलमान बनाने का प्रयास नहीं किया । इसी कारण बाली में अब भी ८० प्रतिशत हिन्दू हैं । पहले यहां के हिन्दू अपने को हिन्दू नहीं कहते थे । क्योंकि भारत के हिन्दू मूर्तिपूजक थे और ये मूर्तिपूजा के विरुद्ध थे । इसी कारण ये अपने को हिन्दू नहीं लिखाते थे । बाद में स्व० आचार्य डॉ. रघुवीर जी ने वहां जाकर इनको बहुत समझाया तो ये अपने को हिन्दू लिखाने लगे । यहां अब 'हिन्दू धर्म परिषद' नाम का एक शक्तिशाली संगठन है । पं० नरेन्द्रदेव ने संध्या की पुस्तकें यहां इण्डोनेशियाई भाषा में छपवाकर बंटवाई हैं । बाली में भी स्वामी जी के कई जगह व्याख्यान व उपदेश हुये ।
बाली से लौटकर स्वामी जी २८ जनवरी को पुनः सिंगापुर पहुंचे । सिंगापुर और इंडोनेशियाई द्वीपों में साधुओं का बड़ा सम्मान है । इस कारण किसी भी हवाई अड्डे पर स्वामी जी की तलाशी नहीं ली गई । जकार्ता से लौटने पर आर्यसमाज सिंगापुर में श्री बाबू जगन्नाथ जी का तार और प्रो० योगानन्द का पत्र मिला, जिनमें ५ मार्च से भारतीय लोकसभा के मध्यावधि चुनाव की चर्चा करते हुये स्वामी जी से तुरन्त स्वदेश लौट आने का आग्रह किया गया था । ४-५ दिन स्वामी जी सिंगापुर में और रहे और दर्जनों स्थानों पर उनके व्याख्यान हुये । चलने से पूर्व आर्यसमाज सिंगापुर के प्रधान श्री दुर्गादास जी सचदेव ने स्वामी जी को एक टेपरिकार्डयुक्त ट्रांजिस्टर (Two-in-One) भेंट किया और ४ फरवरी १९७१ को स्वामी जी अपनी यात्रा पूरी कर सकुशल वापिस स्वदेश लौट आये ।
यहां आने पर अपने एक स्वागत समारोह में स्वामी जी ने सुदूरपूर्व में भारतीय संस्कृति की वस्तुस्थिति का विस्तार से परिचय दिया जो यहां के दैनिक समाचारपत्रों में विस्तार से छपा है । इस समारोह की अध्यक्षता तत्कालीन गृहराज्यमंत्री श्री कृष्णचन्द्र पन्त ने की थी ।
योरोप-यात्रा
स्वामी जी महाराज की चतुर्थ विदेश यात्रा योरोप की थी । सन् १९७३ ई० में पेरिस में "प्राच्यविदों का २९वां अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन" हुआ । उसी में भाग लेने के लिये स्वामी जी गये । डॉ. लोकेशचन्द्र जी भी इनके साथ थे । मुझे भी इस सम्मेलन में शोध-पत्र प्रस्तुत करने के लिये निमन्त्रण मिला । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मार्ग-व्यय देने पर मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से इस सम्मेलन के लिये श्री स्वामी जी महाराज के साथ गया । जम्बो जैट वायुयान द्वारा १४ जुलाई १९७३ को दिल्ली बम्बई से चलकर कुवैत, रोम होते हुये हम अगले दिन फांस की राजधानी पेरिस पहुँचे । यहां का हवाई अड्डा बहुत बड़ा है । पेरिस में हम "सारबोन यूनिवर्सिटी" जहाँ यह सम्मेलन होना था, के निकट लिसबन होटल में रुके । १६ से सम्मेलन आरम्भ हुआ । सम्मेलन स्थल पर ही डॉ. साहब के परिचित एक जिप्सी विद्वान् मिल गये । वह पहले भारत में डॉ. साहब के यहां रहकर कार्य कर चुके हैं । उनसे रोमा जिप्सियों के बारे में जानकारी हुई ।
जिप्सी लोग मध्यकाल में मुसलमानी अत्याचारों से पीड़ित होकर राजस्थान छोड़कर चले गये । ये सब राजस्थान के राजपूत लोग थे । आज भी इनकी बोलचाल की भाषा व वेशभूषा लगभग राजस्थानी ही है । ये लोग भारत से निकल कर ईरान आदि से होते हुये योरोप पहुँच गये । पेरिस के निकट अब इनकी एक बड़ी बस्ती है । फ्रांस में इनकी जनसंख्या ३० हजार के लगभग थी । यह संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है । योरोपवासियों के एक-दो ही बच्चे होते हैं जबकि इनके यहां दस-दस बच्चे होते हैं । फ्रांसीसी इस बात से चिन्तित थे कि कहीं आगे चलकर ये लोग फ्रांस पर पूरा कब्जा ही न कर लें । फ्रांस में हमने अनेक म्यूजियम देखे जिनमें लूव्र म्यूजियम तथा 'म्यूज्ये गिमे' विशेष उल्लेखनीय हैं । लूव्र म्यूजियम में तो हस्तचित्रों पेंटिंग्स (Paintings) का इतना अधिक आढ़्य संग्रह है कि संसारभर में उतना शायद कहीं नहीं होगा । संसारभर के चित्रकारों के चित्र यहां हैं । कलाकारों ने रंग और तूलिकाओं के मेल से जिस कला की सृष्टि की है वह 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' की मुंह बोलती कहानी है । इतने बड़े और भव्य चित्र जिनमें अधिकांश तैलचित्र हैं, हमें योरोपभर में ही नहीं, अमेरिका में भी कहीं देखने को नहीं मिले । पेरिस से हम श्री रविकुमार के साथ 'बारसाई' के राजमहल देखने गये । ये अपनी भव्यता के लिये संसारभर में प्रसिद्ध हैं । इन्हीं महलों से लुई सोलहवें को घसीट कर सन् १७८९ की क्रान्ति के समय फ्रांस की जनता पेरिस ले गई थी और वहीं उसको कैद किया था ।
फ्रांस में एक बात और विशेष देखने को मिली । वह यह कि यहां के ९५ प्रतिशत व्यक्ति अंग्रेजी नहीं जानते या नहीं बोलते । यहां आकर हमारा यह व्यामोह टूट गया कि अंग्रेजी सम्पूर्ण योरोप की भाषा है । विशेषकर सम्मेलन ने तो यह सिद्ध कर ही दिया कि उसके स्थानीय आयोजक अंग्रेजी से घृणा करते हैं । उन्हें अपनी फ्रेंच भाषा पर गर्व है और वे इसे ही बोलते हैं । अपनी राष्ट्रभाषा से उनका यह प्रेम प्रशंसनीय है ।
पेरिस में हमने लगभग सभी दर्शनीय स्थल देखे । संसारप्रसिद्ध एफिल टावर पर भी चढ़े । सम्मेलन में बेल्जियम के एक विद्वान् ने जो उन दिनों आस्ट्रेलिया में प्रोफेसर था, स्वामी दयानन्द पर लेख पढ़ा । स्वामी जी महाराज जान-बूझकर उसका लेख सुनने गये थे । उस विद्वान् ने सत्यार्थप्रकाश के प्रथम तथा द्वितीय संस्करणों में भेद दिखलाकर महर्षि दयानन्द पर कुछ आक्षेप किये । उसका लेख समाप्त होते ही प्रश्नकाल में स्वामी जी खड़े हुये और उससे प्रतिप्रश्न कर तथा तर्कपूर्वक उसकी स्थापना का खंडन कर इन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि उसको जवाब देना कठिन हो गया । ऐसी स्थिति में उस विभाग के अध्यक्ष रूसी विद्वान् चैलीशोफ ने उसका पीछा छुड़ाया और स्वामी जी महाराज से आगे और प्रश्न न करने की प्रार्थना कर उसे बैठा दिया । उस दिन मैं स्वामी जी की तर्कबुद्धि देखकर दंग रह गया । वहां बैठे अनेक विदेशी विद्वानों ने भी इनकी प्रशंसा की । २१ जुलाई को यह सम्मेलन समाप्त हुआ ।
२३ जुलाई को पेरिस से उड़कर १ घंटा बाद हम स्वामी जी के साथ लन्दन पहुँच गये । यहां पांच दिन ठहरकर हमने ब्रिटिश म्यूजियम तथा विक्टोरिया एल्बर्ट म्यूजियम देखे । ब्रिटिश म्यूजियम में पुरातत्त्वीय सामग्री का अथाह संग्रह है । अंग्रेज भारत से कितनी बहुमूल्य निधि उठा ले गये हैं यह वहीं पर हमें ठीक तरह पता चला । यौधेयगण के इतिहास में रुचि और कार्य होने के कारण हमने इनके सिक्के विशेष रूप से देखे । इसके लिये हमें उच्चधिकारियों से विशेष आग्रह करना पड़ा ।
यहां हम एक गुजराती होटल सरूना में ठहरे । तीन दिन तक लगातार हम 'हरे रामा हरे कृष्णा' मन्दिर में भी जाते रहे । लन्दन में इनके कई मन्दिर हैं । यहां योरोप के विभिन्न देशों के ब्रह्मचारी रहते हैं जो भारतीय विद्या का अध्ययन करते हैं और भारतीय साधुओं की ही भांति रहते हैं ।
लन्दन से पश्चिम जर्मनी तथा पूर्वी जर्मनी गये । पूर्वी जर्मनी की राजधानी बर्लिन में इन दिनों "विश्व युवक सम्मेलन" हो रहा था । दुनियां भर के युवक यहां एकत्र थे । विशेष कर जर्मनी की युवक युवतियों ने जब स्वामी जी को देखा तो वे जगह-जगह इनको घेरकर खड़े हो जाते और इनके हाथ में बालपेन थमाकर अपनी बनियानों पर इनके हस्ताक्षर कराते । कोई पीठ पर तो कोई वक्षःस्थल पर । कोई गेंद पर तो कोई अपने गुब्बारे पर । ये अपने इस सम्मेलन की यादगार रखने के लिये ऐसा कर रहे थे । स्वामी जी वहां अत्यधिक श्रद्धा अर्जित कर रहे थे । इस दिन न जाने कितने सौ हस्ताक्षर स्वामी जी ने किये होंगे ।
जर्मनी से नार्वे, डेनमार्क (कोपनहेगन) और स्वीडन दो-दो तीन-तीन दिन ठहरते हुये हम हालेण्ड की राजधानी अमस्टर्डम पहुंचे । यहां डच लोगों का कमाल देखने को मिला । उन्होंने समुद्र पर काबू पा-पाकर किस प्रकार इस शहर का विस्तार किया है यह अपने आप में बहुत दिलचस्प बात है । वे अब भी समुद्र को सीमित करने में जुटे थे ।
हालैंड से हम स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध पर्यटन नगर ज्यूरिख पहुंचे । यहां से डॉ. लोकेशचन्द्र जी हम से अलग चले गये । हम रोम आ गये । रोम में 'वेटिकन सिटी' देखा जो दुनियां की एक अनोखी धार्मिक सल्तनत-सी है । यहां का प्रसिद्ध गिरजाघर भी दर्शनीय है । ईसाइयों का सदियों से यह गढ़ तीर्थस्थल रहा है परन्तु यहां रोम में जितनी अंधेरगर्दी और नैतिक पतन हमें देखने को मिला वह योरोप में अन्यत्र कहीं नहीं । यहां बारगेनिंग बहुत अधिक है । यहां जितने अधिक चर्च, गिरजाघर और पादरी हैं, उतना ही अधिक यहां भ्रष्टाचार है । दो दिन रोम में रहकर हम ९ अगस्त १९७३ को वापिस मातृभूमि पर आ पहुंचे । स्वामी जी का व्यक्तित्व विदेशों में भी कितना प्रभावशाली रहता है यह इस यात्रा में अनेक बार देखा ।
अफ्रीका यात्रा
सन् १९७८ ई० में स्वामी जी महाराज अफ्रीका यात्रा पर गये । आर्यसमाज नैरोबी ने अपनी ७५ वर्षीय हीरक जयन्ती तथा आर्य प्रतिनिधि सभा पूर्वी अफ्रीका ने अपना रजत-जयन्ती समारोह सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के आग्रह पर अन्तर्राष्ट्रीय आर्यसम्मेलन के रूप में परिवर्तित कर दिया । इस सम्मेलन में भाग लेने के लिये भारत भर से लगभग २०० आर्यसमाजी लोग पहुँचे । हरयाणा आर्य प्रतिनिधि सभा के आग्रह पर स्वामी जी भी वहां पहुँचे । हरयाणा से कई आर्य इस सम्मेलन में जाना चाहते थे परन्तु सार्वेदेशिक सभा की ओर से प्रबन्ध ही नहीं किया जा सका । अनेक व्यक्तियों को अपना मार्ग-व्यय आदि वापिस लेना पड़ा ।
नैरोबी में होने वाले इस सम्मेलन के लिये श्री स्वामी जी ने १२ दिसम्बर १९७८ को सायं दिल्ली से और १३ सितम्बर को बम्बई से वायुयान द्वारा प्रस्थान किया । इनके साथ जाने वाले अन्य प्रमुख व्यक्तियों में चौ० हीरासिंह भूतपूर्व कार्यकारी पार्षद दिल्ली, श्री चौ० हरकिशन जी मलिक डिस्ट्रिक्ट सैशन जज दिल्ली, श्री सोमनाथ मरवाह एड्वोकेट और श्री सच्चिदानन्द जी शास्त्री उपमन्त्री सार्वेदेशिक सभा आदि थे ।
इस सम्मेलन में कनाडा, अमेरिका, इंगलैंड आदि अनेक देशों के आर्य प्रतिनिधि भाग ले रहे थे । सम्मेलन के अवसर पर नैरोबी आर्यसमाज की ओर से यजुर्वेद पारायण यज्ञ का आयोजन हुआ । स्वामी जी महाराज के यज्ञ के उपरान्त दो बार उपदेश हुये । विभिन्न सम्मेलनों में भी इनके भाषण हुये ।
नैरोबी आर्यसमाज आज एक धनाढ़्य संस्था है । इसका मन्दिर अति विशाल तथा सुन्दर है । मन्दिर के बाहर की ओर निकाली गई दुकानों से लाखों रुपया प्रतिवर्ष आय होती है । यहां इस देश में अनेक आर्यसमाज हैं । स्त्री आर्यसमाजों का भी अच्छा प्रचार है । आर्यसमाज की ओर से कई शिक्षण संस्थायें भी चलती हैं । ५ जुलाई १९०३ के दिन म० जयगोपाल जी के घर नैरोबी आर्यसमाज की स्थापना हुई थी । उसके बाद यह उत्तरोत्तर उन्नति करता गया । नैरोबी के अतिरिक्त स्वामी जी महाराज आदि ने मुम्बासा की भी यात्रा की । स्वामी जी ने अपनी नैरोबी यात्रा में वहां के संबन्ध में विस्तार से लिखा है । यहां विस्तारभय से अधिक लिखना उचित नहीं । २९ सितंबर को वहां से चलकर ३० सितम्बर १९७८ ई० को स्वामी जी, चौ० हीरासिंह जी व श्री चौ० हरिकिशन जी मलिक वापिस भारत लौट आये । नैरोबी में आर्यसमाज के पुरोहित प्रो० जयदेव वेदालंकार ने इनकी सुविधाओं का बहुत ध्यान रखा ।
| Digital text of the printed book prepared by - Dayanand Deswal दयानन्द देसवाल |
Back to Index स्वामी ओमानन्द सरस्वती का जीवन-चरित
Back to History

