Swami Dayanand Saraswati

Swami Dayanand Saraswati (1824-1883), born on 12th February 1824 (in Tankara in the state of Gujarat, India), was the founder of the Hindu reform organization Arya Samaj, which he established on April 7th 1875, in Bombay India. He also created the 10 principles of Arya Samaj.
His life
Throughout his life, Swami Dayanand preached against many Hindu traditions which he felt were dogmatic and oppressive. These included traditions such as idol worship, caste by birth, and the exclusion of females from the study of the Vedas. One of his main messages was for Hindus to go back to the roots of their religion, which are the Vedas. By doing this, he felt that Hindus would be able to improve the depressive religious, social, political, and economic conditions prevailing in India in his times.
One of Swami Dayanand's major arguments for going back to the Vedas was that, in his own words " the four Vedas, the repositories of knowledge & religious truth, are the Word of God. They are absolutely free of error, & the Supreme & independent authority ". The four Vedas are; Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, & Atharva Veda. To spread awareness of his movement and to revitalize Vedic knowledge, Swami Dayanand published many religious books. These include; Satyartha Prakash ( The light of Truth ), the Rig Vedaadi, Bhasyya- Bhoomika, and Sanskar Vidhi.
Swami Dayanand preached many messages to Hindus during his lifetime. For instance, he preached that Hindus should worship just one, formless, God. He fought against polytheism by telling people the true meaning of the names of God, & established how all of them pointed at one & the same God- Paramathama, the Supreme Self. Further, Swami was " a voice against superstition, against unrighteousness, which reigned supreme in the garb of true religion, and against a foreign rule".
Throughout his known adult life, Swami's main message was " Back to the Vedas ". By this, Swami Dayanand meant that Hindus should stop practising beliefs such as idol worship, caste, polytheism, pantheism, untouchability, child marriages,forced widowhood, and many other practices which he felt were wrong. He challenged many of the Hindu orthodoxy if they could justify their belief in the aforementioned practices. This induced the anger and wrath of many orthodox Hindus, which subsequently led to 14 attempts at poisoning Dayanand. Miraculously, he was able to use his Yogic abilities to cure himself from the first 13 attempts. However, the 14th time proved fatal. Swami Dayanand died, and left the world with his legacy, Arya Samaj.
स्वामी दयानन्द के जीवन पर एक रोचक लेख
यह लम्बा लेख प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी लाला लाजपतराय का लिखा हुआ है जो सबसे पहले सन् 1898 AD में लाहौर में प्रकाशित हुआ था - Dndeswal 01:18, 16 June 2011 (EDT)
स्वामी दयानन्द का आगमन
जिस समय राजा राममोहन राय वेदान्त तथा उपनिषदों के अनुवादों को प्रस्तुत कर हिन्दू धर्म को ईसाइयत के आक्रमणों से बचा रहे थे, काठियावाड़ के एक औदीच्य ब्राह्मण परिवार में एक बालक का पालन हो रहा था जिसके भाग्य में वैदिक धर्म के प्रचार तथा धर्मसुधार का श्रेय अंकित था । जिस समय झुंड के झुंड हिन्दू युवक ईसाई बन रहे थे और हिन्दू जाति में कोलाहल मचा हुआ था, उन्हीं दिनों में एक दण्डी सन्यासी नर्मदा के तटवर्ती जंगलों में तप कर रहा था । उन्हीं दिनों में एक बाल ब्रह्मचारी संन्यासी मथुरा के एक अंध संन्यासी से वैदिक व्याकरण की शिक्षा प्राप्त कर रहा था और अपने आपको उस कार्य के लिये तैयार कर रह था जो उसे आगे चलकर करना था ।
यह ब्राह्मण बालक तथा दण्डी संन्यासी स्वामी दयानन्द थे और जिस प्रज्ञाचक्षु दण्डी ने उसे वैदिक व्याकरण की शिक्षा देकर पुराणों के खण्डन तथा वैदिक धर्म के मण्डन के लिये तैयार किया, वे थे विरजानन्द सरस्वती । धन्य था वह गुरु और धन्य वह शिष्य जिन्होंने वैदिक धर्म की डूबती नौका को सहारा देकर उसे भंवर से निकाला और हिन्दुओं को अधोगति से उबरने का मार्ग दिखलाया ।
स्वामी दयानन्द उस समय उत्पन्न हुए जब हिन्दू लोग मुसलमानी बादशाहत की जीर्ण-शीर्ण इमारत को ठोकर लगाकर भी एक अन्य शक्तिशाली जाति के पंजे में फंसते जा रहे थे । स्वामी जी का पालन पोषण उस समय हुआ जब ब्रह्मसमाज प्राचीन आर्य धर्म के प्रचार के लिए प्रयत्नशील था ऐर ईसाई मत की जड़ भारत में जमती जा रही थी । स्वामी दयानन्द उस समय तपस्यारत थे जब भारत में आत्मिक और राजनैतिक हलचल से समस्त वातावरण व्याप्त था । स्वामीजी उस समय वैदिक व्याकरण के अध्ययन में रत थे जब पंजाब में नवीन शिक्षा प्रणाली का आरम्भ हो रहा था । वे उस समय कर्मक्षेत्र में उतरे जब हिन्दुओं की व्याकुल आत्माएं किसी ऐसे ही महापुरुष के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थीं ।
ऐसी ही आवश्यकता के समय परमात्मा ने उनको यह प्रेरणा दी कि वे वैदिक धर्म की रक्षा करें और भूली-भटकी आर्य जाति को सन्मार्ग पर लायें, मृतप्राय संस्कृत भाषा में नवीन प्राणों का संचार करें और वैदिक साहित्य में नवीन प्रज्ञा को समाविष्ट करें । अतः यह निर्विवाद है कि स्वामी दयानन्द का आगमन वैदिक धर्म, संस्कृत भाषा, वैदिक साहित्य और दर्शन के लिये संजीवनी सिद्ध हुआ ।
दोहा -
भारत दुर्दशा को देखकर दयालु को दया आई ।
महर्षि जिसे भेज के दिया यश और पण्डिताई ॥
स्वामी दयानन्द महापुरुष थे
संसार में लाखों मनुष्य नित्य जन्मते और मरते हैं । सैंकड़ों नवीन आत्मायें नवीन सजधज और शोभा के साथ सृष्टि में आती हैं । उनके जन्म लेने पर अत्यन्त प्रसन्नता प्रकट की जाती है, संसार के समाचारपत्र उनकी प्रशंसा के गीत गाते हैं और उनके माता पिता तथा परिवार के लोगों को बधाईयाँ देते हैं । देश के मन्दिरों में उनकी आयु-वृद्धि के लिये प्रार्थना की जाती है । बड़े-बड़े धर्मनिष्ठ लोग उनकी सफलता के लिये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं । प्रतिक्षण उनकी सुरक्षा के कदम उठाये जाते हैं । प्रतिवर्ष उनकी प्रगति की रिपोर्टें छपती हैं । उनके कार्यों को सृष्टि के अद्भुत कार्यों में गिना जाता है । उनकी उत्पत्ति से ही लोगों के मन में एक अपूर्व आह्लाद पैदा हो जाता है क्योंकि लोगों को उनसे बहुत बहुत आशाएँ होती हैं । परन्तु खेद इस बात का है कि ऐसे लोगों में से अधिसंख्य अपने कार्यों से यह सिद्ध कर देते हैं कि उनका जन्म लेना लोगों के लिये प्रसन्नता का हेतु नहीं था । उनमें से अनेक अपने माता-पिता तथा अपने वंश को कलंकित काने वाले सिद्ध होते हैं तथा मानवता से सर्वथा रहित होते हैं । जब वे मर जाते हैं तो संसार को उनकी मृत्यु से कोई खेद नहीं होता अपितु कई लोग तो उनसे इतनी घृणा करने लगते हैं कि उनकी मौत को पृथ्वी का भार दूर होना ही समझते हैं । लोग यही समझते हैं कि धरती से एक बला टली । दूसरी ओर बहुत कम संख्या में ऐसे लोग भी जन्म लेते हैं जिनके आने की दुनिया को खबर ही नहीं लगती । केवल उनके नाते-रिश्तेदारों को ही उनके जन्म का ज्ञान होता है और उनका आविर्भाव संसार के लिये किसी भी प्रकार महत्त्वपूर्ण नहीं माना जाता । ऐसे लोग पर्याप्त समय तक गुमनामी की ही जिन्दगी जीते हैं और इस अप्रसिद्धि में ही जीवन-यात्रा का कुछ भाग व्यतीत करते हैं । वे अप्रसिद्ध रहकर ही मर जाते हैं । उनका जन्म, जीवन और मृत्यु संसार की कोई प्रसिद्ध घटना नहीं मानी जाती । लोगों को पता ही नहीं चलता कि कौन जन्मा और कौन मरा । अनेक ऐसे भी होते हैं जो अप्रसिद्धि की अवस्था में जन्म लेते हैं, इसी अवस्था में शिक्षा ग्रहण करते हैं किन्तु जब युवा होते हैं तो उनकी गणना प्रसिद्ध लोगों में होती है । समस्त संसार में नहीं तो कम से कम एक प्रान्त में तो वे अपना नाम करते ही हैं । जब उनकी मृत्यु होती है तो अनेक लोग उनके लिये शोक करते हैं और उनके गुणों का स्मरण करते हैं । उनका यश थोड़ा स्थायी होता है । किन्तु एक-दो पीढ़ी के बाद लोग उन्हें भी भूल जाते हैं परन्तु किसी समय विशेष पर ही लोग उन्हें याद करते हैं । इसके अतिरिक्त एक श्रेणी उन लोगों की है जिनकी संख्या अत्यन्त कम है । ये लोग गुमनामी में ही पैदा होते हैं और गुमनामी में ही पलते हैं किन्तु जब कर्मक्षेत्र में आते हैं तो अपने बुद्धि, अन्तश्चेतना, लगन, योग्यता, मनुष्यत्व तथा वीरता के कारण संसार के लोगों को अपनी ओर खींचते हैं । वे लोग संसार में दृढ़ प्रभाव उत्पन्न करते हैं, लोगों में खुद के लिए आकर्षण पैदा करते हैं । कार्लाइल ने ऐसे मनुष्यों की उपमा अग्नि के स्फुलिंगों से दी है जिन्हें लोग परमात्मा कहते हैं । ऐसे मनुष्य पृथ्वी को प्रकाशित करने के लिये सूर्य तुल्य हैं । वे सूर्य के तुल्य ही यश पाते हैं और संसार को उनसे प्रकाश मिलता है । उनकी मृत्यु मनुष्य जाति के एक सीमित वर्ग के लिये ही नहीं, बल्कि समस्त मानव-जाति के लिए खेदजनक होती है । उनका नाम कभी नहीं मरता और उनका काम कभी नष्ट नहीं होता । उनकी याद कुछ दिनों या कुछ शताब्दियों में भी विलीन नहीं होती, किन्तु वह सदा तरोताजा रहती है । उनके द्वारा फैलाई गई ज्योति एक काल या एक पीढ़ी को ही प्रकाशित नहीं करती, किन्तु उसका प्रभाव सदा के लिए जगत् में रहता है । उनकी कार्यप्रणाली एक वंश या एक समय तक ही स्मरणीय नहीं रहती, अपितु उस पर सदा चर्चा और वाद-विवाद होता रहता है । ऐसे मनुष्यों का आचरण ही संसार में महत्त्वपूर्ण होता है । ऐसे मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं । संसार में अन्य लोगों के लिये वे प्रकाशस्तम्भ तुल्य होते हैं । संसार के महावन में वे विश्रामस्थल के समान होते हैं । विश्व के राजमार्ग पर मील के पत्थर के तुल्य होते हैं जिन पर यात्रा की मंजिलें अंकित रहती हैं । ऐसे लोग आत्मिक क्षुधातुरों तथा तृषा से व्याकुल पुरुषों के लिए भोजनागार तथा जलाशय के तुल्य हैं । लोग उनके व्याख्यान सुनकर ही अपनी आत्मा का आहार पाते हैं और व्याकुलता को शान्त करते हैं । आप चाहे उन्हें अवतार कहें या पैगम्बर, ईश्वर का स्थानापन्न कोई ऋषि-महर्षि कहें अथवा महापुरुष कहकर पुकारें, वे एक की शिला के खण्ड, एक ही अग्नि के स्फुलिंग, एक ही कारखाने के पहिये और एक ही कल के पुर्जे होते हैं । संसार का कोई भाग ऐसे मनुष्यों के अस्तित्व से खाली नहीं होता । भगवान् कृष्ण, महात्मा बुद्ध, महर्षि व्यास, गौतम, कणाद, जैमिनि, कपिल और पतञ्जलि आदि इसी श्रेणी के मनुष्य थे । स्वामी शंकराचार्य, गुरु नानकदेव, गुरु गोविन्द सिंह भी इसी कोटि के थे । महाराज विक्रमादित्य, सम्राट् अशोक तथा शिवाजी महाराज भी ऐसे ही महापुरुष थे । हमने केवल नमूने के रूप में ये नाम लिखे हैं ।
हमारा दृढ़ विश्वास है कि स्वामी दयानन्द भी इसी श्रेणी के महापुरुष थे । अप्रसिद्धि में जन्मे, उसी रूप में पले, शिक्षा-प्राप्ति तक भी अप्रसिद्ध ही रहे, किन्तु जब कर्मक्षेत्र में आये तो जीवनपर्यन्त सिंह की तरह गरजते रहे । स्वामी जी ने एक पुरातन जाति को मृत्यु की स्थिति से हटा कर आशा के आसन पर ला बिठाया । एक महान् धर्म को गड्ढ़े से निकालकर प्रकाश के उच्च शिखर पर स्थापित कर दिया । संस्कृत जैसी गौरवमयी भाषा को अप्रसिद्धि की हालत से हटा कर संसार की भाषाओं में प्रधान स्थान दिला दिया । संसार की सभ्यता को गतानुगति से हटा कर सचेत किया । प्रत्येक प्रकार से देखें तो स्वामी दयानन्द महापुरुष सिद्ध होते हैं । यदि शारीरिक दृष्टि से देखें तब भी स्वामी जी महान् प्रतीत होते हैं । वे शरीर से दुर्बल लोगों को सदा तुच्छ मानते थे । शारीरिक बल तथा इन्द्रिय दमन में वे अद्वितीय थे । जीवन से मृत्युपर्यन्त उन्होंने कभी नारी का सान्निध्य नहीं किया । उनके अखण्ड ब्रह्मचर्य पर उनके बड़े से बड़े शत्रु ने भी शंका नहीं की, न उनके जीवनकाल में और न उनकी मृत्यु के पश्चात् ।
स्वामी जी उच्च कोटि के विरक्त और वीतराग पुरुष थे । उन्होंने अपने पिता की सम्पत्ति को लात मारी । जीवन में ऐसे अनेक अवसर आये जब उन्हें अपरिमित धन तथा ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने के प्रलोभन दिये गये किन्तु वे इससे सर्वथा असंपृक्त रहे । उनमें तीव्र बुद्धि तथा अपूर्व स्मरण शक्ति थी । उनके समकालीनों में उनकी सी तीक्ष्ण बुद्धि वाला शायद ही कोई रहा हो । विद्या और चारित्रिक श्रेष्ठता में वे अद्वितीय थे । संस्कृत ज्ञान में उनका कोई सानी नहीं था । निर्भयता में अद्वितीय थे । वे अपने विश्वास पर आजीवन दृढ़ रहे । एक समय ऐसा था जब सारा संसार एक ओर था और स्वामी दयानन्द एक ओर थे । अपने विश्वास को व्यक्त करने तथा विचारों क प्रचार करने में उनके तुल्य अन्य कोई नहीं था । उनको न राजा का भय था और न प्रजा का । वे अपने परिजनों या जाति वालों से कभी भयभीत नहीं हुए और न इतर जाति वालों से । अनथक परिश्रम करने से कभी विरत नहीं हुए । यदि उनके सार्वजनिक जीवन के उस स्वल्प काल ला लेखा-जोखा किया जाए तो उनकी कर्मठता का पूर्ण प्रमाण मिल जाता है । उनकी वाणी और लेखन तथा शास्त्रार्थ कौशल सब कुछ असाधारण था । लोगों को अपनी ओर आकृष्ठ करने की उनमें अद्भुत शक्ति थी । जो मनुष्य उनके समक्ष आता, उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता । वे उच्च कोटि के योगी थे किन्तु उनमें अपने योग बल का स्वल्प भी अभिमान नहीं था ।
योग शक्ति का अभिमान करना तो दूर, वे इसे प्रकट करने में भी संकोच करते थे । कठिनाइयों से कभी घबराये नहीं बल्कि साहस और वीरतापूर्वक उनका सामना किया । न किसी की मित्रता की परवाह की और किसी की शत्रुता की चिंता, अपितु हुआ यह कि अनेक शत्रु उनके मित्र बन गये और मित्र शत्रुवत् आचरण करने लगे । तथापि उस महापुरुष के कार्य और व्यवहार में थोड़ा भी अन्तर नहीं आया । सारांश यह कि स्वामी जी में महापुरुषों के सभी गुण विद्यमान थे । उनके समग्र कार्यों का मूल्यांकन करने का अभी उचित समय नहीं आया है किन्तु हमारा विश्वास है कि एक समय आएगा जब उनके नाम से सारा संसार परिचित हो जाएगा । संस्कृत पृथ्वी की समस्त भाषाओं में वरिष्ठ पद प्राप्त करेगी तो विश्व के लोग उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में उच्च पद पर प्रतिष्ठित करेंगे । उनके मिशन और कार्य को भी आदर की दृष्टि से देखा जाएगा ।
स्वामी दयानन्द का काम
स्वामीजी अभी बालक ही थे जब उन्हें यह बोध हो गया था कि मूर्तिपूजा ईश्वरोपासना का वास्तविक मार्ग नहीं है अपितु यह निकृष्ट कोटि का भ्रष्टाचार है । यह विचार दृढ़ता से उनके मन में जम गया और जीवन में वे इसे कभी छोड़ नहीं सके । अपने माता-पिता के सामने ही उन्होंने मूर्तिपूजा का खण्डन किया और अपने पिता के क्रोधित होने पर भी वे अपने विश्वास को छिपा नहीं सके, जबकि पिता का क्रोध बालक के लिये भयजनक होता है । ब्रह्मचर्य काल और पुनः संन्यास ले लेने पर भी उन्होंने मूर्तिपूजा विषयक अपनी धारणा को कभी गुप्त नहीं रखा । न तो वे किसी यति-मण्डल से डरे और न मण्डलेश्वरों से । वे न राजा से भयभीत हुए और न किसी पण्डित से । जब तक जिये उसी सिंह-गर्जना से मूर्तिपूजा का खण्डन करते रहे । लोगों को मूर्तिपूजा से विरत कर निराकारोपासना की ओर प्रेरित करना उनके जीवन का महत् उद्देश्य था और प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि जो प्रकाश उन्होंने बचपन में ग्रहण किया उसे वीरता और साहस से जीवन्तपर्यन्त बुझने नहीं दिया । प्रत्येक हिन्दू जानता है कि उपनिषदों के काल के पश्चात् भारत में इतना साहसी, निर्भय और मूर्तिपूजा का कट्टर शत्रु दयानन्द के अतिरिक्त कोई और उत्पन्न नहीं हुआ । सभी मतावलम्बी चाहे वे ईसाई, मुसलमान, पौराणिक, वेदान्ती अथवा बौद्ध ही क्यों न हों, इस बात को जानते हैं कि मूर्तिपूजा के प्रति श्रद्धा का भाव उनके मन में कभी उत्पन्न नहीं हुआ । मूर्तिपूजा का खण्डन करने के ही कारण उनके सजातीयों ने, अपनी ही भाषा बोलने वालों ने, स्वधर्म वालों ने, साधारण लोगों ने ही नहीं, अपितु विद्वानों ने भी उन्हें नास्तिक बताया । कोई उन्हें पादरियों का वैतनिक नौकर बताता तो किसी ने उन्हें धर्म का शत्रु कहा, परन्तु इस पुरुष-सिंह ने इसकी थोड़ी भी परवाह नहीं की ।
कई बार उनके सजातीय पण्डितों ने प्रत्यक्ष तथा परोक्ष में भी उनसे प्रार्थना की कि यदि वे मूर्तिपूजा का खण्डन छोड़ दें तो वे उन्हें विष्णु का अवतार घोषित कर देंगे ताकि उनकी सर्वत्र पूजा हो । परन्तु उस महापुरुष पर इन प्रलोभनों का कोई असर नहीं हुआ । वह एक ऐसे दृढ़ आसन पर बैठे थे जहाँ से उन्हें कोई हिला नहीं सकता था । अनेक सामन्तों, राजाओं तथा महाराजों ने उन्हें गुप्त तथा प्रत्यक्ष सम्मति दी थी कि वे मूर्तिपूजा का खण्डन छोड़ दें । उन्हें अनेक प्रकार के लोभ-लालच दिये गये, प्राणों का भय, बदनामी का डर दिखाया, धमकियाँ भी दी गईं, किन्तु उनके दृढ़ हृदय पर कोई असर नहीं हुआ । उन्होंने जिस स्थान पर, जिस दिशा में और जिस रीति से मूर्तिपूजा को देखा, उसका खण्डन उतनी ही निडरता से किया । जड़ पूजा का विरोध उनके हृदय में पत्थर की रेखा की भाँति अंकित था जिसे मिटाने का सामर्थ्य किसी में नहीं था । यह एक ऐसा विषय था जिस पर उन्हें संसार में किसी की परवाह नहीं थी । काशी के 300 पण्डित, कलकत्ता के विद्वान् और नदिया (नवद्वीप) के दार्शनिक भी उनको इस आसन से हटा नहीं सके । जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, इन्दौर और बनारस के राजाओं के प्रयत्न भी व्यर्थ गये । मुसलमान और ईसाई प्रकटतया मूर्तिपूजा के शत्रु हैं किन्तु इनके धर्म में भी उन्होंने मूर्तिपूजा का जितना अंश देखा उसका साहसपूर्वक खण्डन किया । स्वामी दयानन्द का विश्वास था कि मूर्तिपूजा बुद्धिवाद के तो विरुद्ध है ही, वेदों में भी उसका निषेध है तथा वह ईश्वर के प्रकृत ज्ञान के विरुद्ध है । उनकी पक्की धारणा थी कि मूर्तिपूजा धर्म और शिष्टाचार के भी विरुद्ध है और राजनैतिक दासता तथा संसार में असम्मान इसके आवश्यक परिणाम हैं । वह समझते थे कि जब तक हिन्दू लोग मूर्तिपूजा से विरत नहीं होंगे तब तक न तो वे सत्यपक्ष पर चलेंगे और न उनकी राजनैतिक तथा सामाजिक उन्नति ही होगी । इसलिये उन्होंने अपनी आत्मा का समस्त बल मूर्तिपूजा के खण्डन में तथा उसे वेद एवं युक्ति के विरुद्ध सिद्ध करने में लगाया । कौन नहीं जानता कि उन्होंने बड़े-बड़े मूर्तिपूजकों के दिल हिला दिये थे । उन्होंने हिन्दू जाति रूपी स्थिर जल में हलचल पैदा की और हिन्दू पण्डितों को विवश किया कि वे मूर्तिपूजा के समर्थन में वेदों के प्रमाण तलाश करें ।
स्वामीजी वेदों को पूर्ण ज्ञान मानते थे और यदि मूर्तिपूजा का प्रमाण उन्हें वेदों में मिल जाता तो शायद उनका समाधान भी हो जाता, किन्तु ऐसा होना असम्भव ही था । सत्य तो यह है कि मूर्तिपूजा तथा मिथ्या देवपूजा के खण्डन में स्वामीजी ने जो काम किया उसे करने में शंकराचार्य भी असमर्थ रहे थे । हिन्दू धर्म के शत्रु हिन्दू धर्म को मूर्तिपूजक कहकर उस पर आक्रमण करते थे । अब मूर्तिपूजा को हिन्दू धर्म की मौलिक अवधारणा के विरुद्ध सिद्ध कर स्वामीजी ने इन शत्रुओं के हाथ से यह हथियार छीन लिया । मुसलमान और ईसाइयों की वैदिक धर्म के प्रति जो दूषित धारणा थी वह स्वामीजी की शिक्षाओं से छिन्न-भिन्न हो गई । उनमें अब इतनी शक्ति ही नहीं रही कि हिन्दू धर्म को मूर्तिपूजा का धर्म बतलाकर हिन्दुओं को बहका सकें और अपने सम्प्रदाय में मिला सकें । उनके आक्रमणों की रीढ़ ही टूट गई । स्वामीजी ने मूर्तिपूजा को वास्तविक ईश्वर-पूजा से भिन्न सिद्ध कर परकीयों के हमलों को व्यर्थ कर दिया । लाखों मनुष्यों को स्वधर्म-त्याग के पाप से बचाया । यदि वे अपने जीवन में और कुछ भी नहीं करते और केवल यही एक काम (मूर्तिपूजा का खण्डन) करते तब भी वे महापुरुषों की श्रेणी में गिने जाते । परन्तु उन्होंने अन्य भी महान् कार्य किये थे, जिनका वर्णन हम आगे करेंगे । तथापि यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि मूर्तिपूजा का खण्डन स्वामी दयानन्द के जीवन का मुख्य उद्देश्य था ।
स्वामीजी का दूसरा कार्य था हिन्दुओं को रूढ़िवादी ब्राह्मणों द्वारा निर्मित कारागार से मुक्त कराना । उन्होंने आर्यों की श्रेष्ठ बुद्धि को वरीयता प्रदान की और उसे तीव्र बनाने के लिये वेदमंत्रों का ज्ञान दिया । तत्कालीन आर्यों की बुद्दि कुण्ठित हो चुकी थी, किसी में सामर्थ्य नहीं था कि वह उसे इस जकड़न से मुक्त करता । इस कुण्ठित बुद्धि से उन्हें तभी छुटकारा मिलता यदि वे स्वधर्म का त्याग कर देते । लोग स्वहित का चिन्तन करना भी भूल गये थे । तथाकथित निम्न वर्ग के लोगों को तो शिक्षित होने का अधिकार भी नहीं था । यदि शूद्र भूल से भी वेदमंत्रों को सुन लेता तो उसके कानों में पिघला सीसा डालने की आज्ञा थी । स्वामीजी ने उन्हें वेदमंत्र पढ़ने और सीखने की आज्ञा दी तथा बंधनमुक्त किया । उन्होंने समस्त आर्य सन्तान को गायत्री की शिक्षा दी और लोगों को बताया कि शिक्षा से भी बढ़ कर प्रार्थना बुद्धि की शुद्धता की है, जो हमें परमात्मा से करनी चाहिए ।
स्वामीजी ने लोगों को समझाया कि मनुष्य का सर्वोत्तम गुरु तो परमात्मा ही है जिसकी शिक्षा में न तो त्रुटि है और न पक्षपात । परमात्मा ने जब अपने पुत्र (मानव) को संसार में भेजा तो उसे जीवन-यात्रा का निर्भय मार्ग भी बताया । यह शिक्षा सृष्टि के आरम्भ में दी गई थी जिससे मनुष्य बुद्धि की सहायता से मार्गदर्शन प्राप्त करे । स्वामीजी ने आर्यों को बताया कि संसार में जो ज्ञान और सच्चाई दिखाई देती है उसका आदि कारण परमात्मा ही है क्योंकि वही आदि गुरु भी है । उस आदि गुरु ने जो शिक्षा दी वह वेदमंत्रों में वर्णित है और वेद ही मानव मात्र का सर्वस्व हैं । मनुष्यों को इन वेदों को पढ़ने तथा उनसे शिक्षित होने का अधिकार है । उस आदि गुरु की शिक्षा और उसे ग्रहण करने वाली जीवात्मा के बीच कोई पर्दा या अवरोध नहीं है । मनुष्य और ईश्वर के ज्ञान के बीच में जो कृत्रिम बाधायें स्वार्थवश खड़ी की गईं थीं उन्हें स्वामीजी ने समाप्त किया और सबको ईश्वरीय ज्ञान की ज्योति दिखलाई । लोगों को ज्ञान के उस स्रोत से परिचित कराया जिससे नाना विज्ञानों की नहरें निकलती हैं । मनुष्य को उस शाश्वत ज्योति की झलक दिखा दी जिससे संसार के समस्त ज्ञान रूपी दीपक अपना प्रकाश ग्रहण करते हैं और अंधकार को दूर करते हैं । स्वामीजी के जीवन का यह एक महान् कार्य था । हठ और पक्षपात के कारण से जो सर्वसाधारण को वेदों की शिक्षा देने के विरोधी थे तथा स्वयं भी इस ज्ञान से अपरिचित थे, उन्हें स्वामीजी ने वैदिक ज्ञान से परिचित कराया । यों कहने के लिये सभी कहते थे कि हमारा धर्म वेदों पर आधारित है, ब्राह्मण तो यह बात कहते ही थे । किन्तु सच पूछो तो न तो उन ब्राह्मणों को और न सर्वसाधारण को ही इस बात का पता था कि इन वेदों में क्या है तथा उनकी शिक्षा क्या है ।
1862 में मुम्बई हाईकोर्ट में एक लायबल केस (मानहानि) दायर किया गया था । इसका कारण यह था कि ‘सत्यप्रकाश’ नामक एक पत्र ने वल्लभ सम्प्रदाय के तत्कालीन आचार्य की चरित्रहीनता को लेकर एक समाचार प्रकाशित किया था । उसमें यह सवाल उठाया गया था कि दुराचार और व्यभिचार की शिक्षा हिन्दुओं के प्राचीन धर्म से तो अनुमोदित नहीं है, किन्तु वल्लभ सम्प्रदाय के गुरु इन्हीं दुराचारों के पुञ्ज हैं, अतः इस सम्प्रदाय की नवीनता तथा इसमें प्रचलित पाखण्ड स्वतः सिद्ध हैं । इस लेख को अपनी बदनामी का कारण मानकर उक्त सम्प्रदाय के एक गुरु ने पत्र पर मानहानि का अभियोग दायर किया । समाचार के लेखक ने वेदों का सहारा लिया था और कहा था कि हिन्दुओं के धर्म की मौलिक शिक्षाएँ वेदों में ही हैं । किन्तु वादी और प्रतिवादी दोनों को ही पता नहीं था कि वास्तव में वेदों में क्या है । अपने बयान में वादी ने वेद, शास्त्र और पुराणों को हिन्दू धर्म के मान्य ग्रन्थ ठहराया किन्तु उसे स्वीकार करना पड़ा कि वह वेदों तथा ब्राह्मण ग्रन्थों के नाम भी नहीं जानता । वल्लभ सम्प्रदाय का वह गुरु अपने मान्य शास्त्रों के नाम भी नहीं बता सका, यह मूर्खता की पराकाष्ठा थी ।
स्वामी दयानन्द के जीवन में भी ऐसे प्रसंग आये हैं जिनसे हिन्दुओं के वेद विषयक अज्ञान का पता चलता है । काशी में जब स्वामी विशुद्धानन्द और बालशास्त्री जैसे विद्वान् अन्य सैंकड़ों पण्डितों को साथ लेकर स्वामीजी से शास्त्रार्थ करने के लिये आये तो उन्होंने मंत्र भाग की जगह गुह्य सूत्रों के कुछ पन्ने उनके हाथ में दे दिये और उन्हें ही वेद कहा । उस समय की बात को जाने दें । सनातन धर्म सभा लाहौर तो आज भी यह मानती है कि पुराण वेदों की ही भाँति ईश्वर रचित हैं तथा उनकी रचना भी वेदों जितनी पुरानी है । यह तब है जब एक साधारण संस्कृतज्ञ भी जानता है कि वेदों के ईश्वरप्रणीत होने के बारे में लोगों का कुछ भी विचार हो, उनके काल के सम्बन्ध में तो कोई सन्देह है ही नहीं । स्वामी दयानन्द के काल के पहले ही यूरोप के संस्कृतज्ञ यह स्पष्ट कर चुके थे कि हिन्दू विद्वानों ने पुराणों के ईश्वरप्रणीत होने की बात कभी नहीं कही । प्रो० गोल्डस्टुकर ने एक स्थान पर ठीक ही लिखा है –
- “जब कोई जाति अपने धर्माचार्यों के बहकाने से अथवा अविद्या के कारण पुराणों जैसी नवीन पुस्तकों को ईश्वरीय ज्ञान कहने लगे तो उसका नतीजा उस जाति के घोर अधःपतन का ही होगा, जिससे उठना कठिन है । हिन्दू जाति पतन की उसी सीमा तक पहुंच गई है और देखना है कि उसके कदम अब किस ओर उठते हैं । माना कि वह कई शताब्दियों से उसी स्थान पर खड़ी है किन्तु वर्तमान समय की राजनैतिक और सामाजिक दशा उसे एक स्थान पर खड़ा नहीं रहने देगी । जब से हिन्दुओं ने पुराणों को अपना धर्मस्रोत बताना आरम्भ किया, तब से धार्मिक प्रवञ्चना के मार्ग की बाधायें दूर हो गईं और ऐसे सम्प्रदाय उत्पन्न हो गये जिन्होंने धर्म और समाज को नष्ट कर दिया । ऐसे-ऐसे नियम बने जो सर्वथा लज्जाजनक थे । ऐसी-ऐसी प्रथायें जारी की गईं जो हिन्दुओं के लिये चिन्ता तथा लज्जा का कारण बनीं । यहाँ इस बात की आवश्यकता नहीं है कि विस्तार में जाकर इन प्रथाओं की हम समीक्षा करें । इस प्रसंग में तंत्र साहित्य की कलई खोली जा सकती है किन्तु इस समय कलकत्ता, बम्बई तथा बनारस से जो पत्र प्रकाशित होते हैं उनसे स्पष्ट हो जाता है कि पुराण और तंत्र साहित्य कितना विषाक्त है । तथापि इन ग्रन्थों के आलोचक आज के विद्वान् भी हिन्दू जाति के समक्ष उत्पन्न खतरे का मुकाबला करने में असमर्थ हैं । ऐसा वे तब ही कर सकेंगे जब वे साहस के साथ रोग का निदान करेंगे और हिन्दुओं को इन दूषित ग्रन्थों से बचा पायेंगे ।”
यूरोप के धर्मसुधार का संदर्भ देकर उक्त लेखक (प्रो० गोल्डस्टुकर ) लिखते हैं - “इस बुराई को रोकने का एकमात्र उपाय यही है कि सर्वसाधारण को उन मूल ग्रन्थों को देखने की इजाजत हो जो आज ब्राह्मण जाति के एक अल्पांश के अधिकार में है । ये ही उसका अर्थ जानते हैं । इसी वैदिक साहित्य को हिन्दुओं को पढ़ना चाहिए ताकि उन्हें मालूम हो कि उनके धर्म का वास्तविक मूल न ब्राह्मण ग्रन्थ हैं और न पुराण, बल्कि वह है ऋग्वेद ।”
हम यह जानते हैं कि उक्त प्रोफेसर की इस अपील को कलकत्ता, बम्बई तथा काशी के पण्डितों ने अनसुना कर दिया । यदि किसी मनुष्य के हृदय में ये विचार उत्पन्न हुए और उसने इन्हीं विचारों को आधार बना कर हिन्दू धर्म के सुधार का कार्य किया तो वे स्वामी दयानन्द ही थे । स्वामीजी ने युक्ति, प्रमाण तथा ऐतिह्य के प्रमाणों से सिद्ध कर्दियाकि पुराण हिन्दुओं को ईश्वरप्रदत्त ग्रन्थ नहीं हो सकते और न हैं । जो कोई पुराणों के प्रतिपाद्य को पढ़ेगा वह स्वामीजी की इस व्यवस्था को स्वीकार करेगा । उन्होंने सिद्ध कर दिया कि हिन्दुओं के ईश्वरीय ग्रन्थ वेद संहितायें हैं न कि पुराण, धर्मशास्त्र, उपनिषद अथवा ब्राह्मण । उन्होंने यह भी प्रमाणित किया कि यद्यपि उपनिषद, ब्राह्मण तथा धर्मशास्त्र ऋषिप्रणीत हैं किन्तु वे वेदों पर ही निर्भर हैं और उनकी मान्यता तभी तक है जहाँ तक वे वेदानुकूल तथा वेदों से अविरुद्ध हैं । सिद्धान्त यह है कि केवल चार वेद ही ईश्वरीय ज्ञान हैं । इन्हीं पर वैदिक धर्म का आधार है और ये ही हमारे लिये अन्तिम प्रमाण हैं । शास्त्रकारों के अनुसार वे ही स्वतः प्रमाण हैं, सत्य शास्त्र हैं जिनमें सत्य के सिवाय कुछ नहीं है ।
स्वामी दयानन्द के जीवन का द्वितीय महान् कार्य
स्वामीजी ने हमको यह तो बताया कि वेद ही ईश्वरीय ज्ञान के ग्रन्थ हैं किन्तु जब तक कि इस वेदार्थ की वास्तविक प्रणाली को नहीं समझ लेते तब तक यह ग्रन्थ हमारे किसी काम के नहीं थे । उन्होंने यह अनुभव किया कि वेदों की संस्कृत और वेद भाष्यकारों के युग की संस्कृत में कितना अन्तर आ गया था । उन्होंने जान लिया कि इन भाष्यकारों ने वेदों की भाषा को समझने तथा उसका अनुवाद करने में क्या-क्या भूलें की हैं । इन भूलों का कारण यह था कि उन्होंने वैदिक संस्कृत को भी आधुनिक संस्कृत के नियमों से ही पढ़ा और उसे समझने में महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों को ओझल किया । वेदों पर आजकल सायण के भाष्य को ही प्रामाणिक माना जाता है जिसका समय यूरोपीय विद्वानों के अनुसार 500 वर्ष पुराना है । सायण मुसलमानी समय में हुआ था । उसकी रचना (भाष्य) पर पौराणिक छाया है । सायण पौराणिक देवपूजा पद्धति को मानता था जबकि महीधर तांत्रिक था । दोनों ने वेदभाष्य करते समय निरुक्त की उपेक्षा की । दोनों ने प्रचलित संस्कृत के नियमों से ही वेदार्थ किया । दोनों ने इस सिद्धान्त को दृष्टि से हटा दिया कि वेदों के शब्द यौगिक हैं और उनके वास्तविक अर्थ तभी प्राप्त हो सकते हैं जब उन्हीं नियमों से उनका अर्थ किया जाए । इन दोनों ने पाणिनीय व्याकरण, निरुक्त तथा निघण्टु की उपेक्षा करके ही वेदभाष्य किया । जिन मंत्रों का उपनिषद् तथा ब्राह्मण ग्रन्थों के लेखकों ने अर्थ कर दिया था, उन अर्थों की भी अवज्ञा कर अपने नये अर्थ किये । परिणाम वही निकला कि अर्थ का अनर्थ हो गया । वेदों को ईश्वरीय मान कर भी उन्हें साधारण पुस्तकों की कोटि से भी गिरा दिया । जिस समय वेदों के ज्ञान का पूर्ण अभाव था, उस समय लोगों ने सायण और महीधर के भाष्यों को ही पढ़ा और मंत्रों के अर्थ का पूर्ण बोध न हो सकने के कारण उन्हें सर्वथा अचिंतनीय मान लिया । उन्होंने ऐसे ग्रन्थों को ईश्वर का ज्ञान मानना तो अस्वीकार किया ही, इन्हें सामान्य महत्त्व भी नहीं दिया । ब्रह्मसमाज ने यह जानने के लिये कि वेदों में क्या है, चार युवा ब्राह्मणों को वेद पढ़ने के लिये काशी भेजा और उनकी साक्षी से यह घोषित कर दिया कि वेद ईश्वर वाक्य नहीं है । राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्मसमाज ने इन्हीं ब्राह्मणों के कहने में आकर स्वयं राजा साहब तथा प्राचीन ऋषियों की वेद विषयक मान्यता को नकार दिया । पहले तो यूरोपीय विद्वानों ने भी सायण और महीधर के आधार पर ही वेदों के विषय में अपने सम्मति दी थी, किन्तु वे शीघ्र ही यह समझ गये कि वेदार्थ ज्ञान के लिये सायण और महीधर की सहायता लेना निरापद नहीं है । किन्तु आर्यावर्त में किसी पण्डित ने यह साहस नहीं दिखाया कि सायण के भाष्य को एक ओर रख कर वेदों का सत्यार्थ करे । इसके कई कारण थे । प्रथम तो यह कि ब्राह्मण लोग ही विचारशक्ति से हीन थे । वे लकीर के फकीर बने हुए थे और किसी ने चिन्तन के क्षेत्र में क्रान्ति लाने का साहस नहीं था । वे तो उसी मार्ग पर चल रहे थे जिसे उन्होंने कई शताब्दियों पूर्व अपना लिया था । इस परम्परागत पथ से थोड़ा भी हटने का साहस उनमें नहीं था । यदि उन सदियों में स्वामी दयानन्द जैसा कोई व्यक्ति उत्पन्न भी होता तो युग की परिस्थितियाँ उसे आगे बढ़ने नहीं देतीं । सत्य तो यह है कि लोग जिस रास्ते पर सदियों से चल रहे थे उसे ही वे निरापद समझ बैठे थे । यदि उन विगत वर्षों में स्वामी विरजानन्द जैसा कोई क्रान्तिकारी उत्पन्न भी होता तो वह भी युगजन्य विवशताओं के कारण इच्छित कार्य करने में असमर्थ ही रहता । सत्य तो यह है कि शंकर स्वामी के पश्चात् स्वामी दयानन्द के अतिरिक्त किसी का भी साहस नहीं हुआ कि सायण और महीधर को एक ओर रख कर वेदार्थ करे । स्वामीजी की तो यह दृढ़ धारणा थी कि हिन्दुओं की बुद्धिहीनता तभी दूर होगी जब वे मध्यकालीन पण्डितों की अंध धारणाओं से अपने को मुक्त करेंगे । यह साहस का कार्य उन्होंने ही किया और स्वबुद्धि के अनुसार ईश्वरीय ज्ञान वेदों को सर्वसाधारण तक पहुंचाया । दो हजार वर्षों के पश्चात् उन्होंने हिन्दुओं को समझाया कि वेदों में प्रयुक्त इन्द्र, अग्नि और वायु आदि नाम परमात्मा के ही हैं । वेदों का व्याकरण अष्टाध्यायी ही है और वेदार्थ को जानने के लिये सायण और महीधर को मार्गदर्शक मान लेना उचित नहीं है । वेद के वास्तविक अध्यापक तो निरुक्त, निघण्टु, उपनिषद् तथा ब्राह्मण ही हैं । दो हजार वर्षों के बाद स्वामीजी ने प्रथम बार हिन्दुओं को यज्ञ, देवता आदि शब्दों के वास्तविक अर्थ बताये । यह भी बताया कि वैदिक साहित्य में ये शब्द जहाँ आये हैं वहाँ उनका क्या अर्थ करना चाहिए । परिणाम यह हुआ कि हिन्दुओं ने स्वामीजी की विद्वत्ता के प्रभाव को स्वीकार किया । आज तक वेदों का यह प्रकृत अर्थ कोई नहीं कर सका था अतः इस कार्य में उनके साहस को देख कर लोग चकित रह गये । यद्यपि अनेक लोगों ने उनके भाष्य को नहीं माना किन्तु किसी को उसमें दोष निकालने का साहस नहीं हुआ । यूरोपीय विद्वानों ने इसका लाभ अवश्य उठाया और वह इस प्रकार कि इस विषय में पहले जो सन्देह थे वे अब निश्चय में बदल गये । उन्होंने सायण भाष्य को अविलम्ब अप्रामाणिक मान लिया । अब वे स्वतंत्र रीति से वेदों का अर्थ करने लगे । यद्यपि यह स्मरणीय है कि यूरोपीय विद्वानों की प्राचीन संस्कृत भाषा तथा पुरातन ग्रन्थों में पूरी गति नहीं थी । सच कहें तो अभी वे इस विषय के प्रारम्भिक विद्यार्थी ही थे । संस्कृत कोई ऐसी भाषा नहीं है जिस पर थोड़े समय में ही अधिकार प्राप्त किया जा सके । इसलिये यूरोपीयों द्वारा किये हुए वेदानुवाद हिन्दुओं के लिये विशेष उपयोगी नहीं थे । प्रो० मैक्समूलर ने ऋग्वेद के कुछ मंत्रों का अनुवाद प्रकाशित किया था । इसकी द्वितीयावृत्ति अभी हाल में निकली है । दोनों की तुलना से यह स्पष्ट हो जाता है कि यूरोपीय विद्वानों की वेद विषयक सम्मति में कितने परिवर्तन हो रहे हैं । इस अनुवाद की भूमिका में प्रोफेसर साहब खुद स्वीकार करते हैं कि सौ वर्षों के अविरल परिश्रम के पश्चात् यूरोपीय विद्वान इस योग्य हुए हैं कि वे अनेक मंत्रों के अर्थ को जान पाये हैं । इस प्रकार प्रो० मैक्समूलर की सम्मति में वेदों की भाषा को समझने में समय अपेक्षित है । उसको समझना पहेलियां बूझने के समान है । वे ठीक कहते हैं कि वेदों के सत्यार्थ तक पहुंचने के लिये सदियों तक यत्न करना होगा क्योंकि इस भाषा में विगत हजारों वर्षों में अनेक परिवर्तन हुए हैं । इन परिवर्तनों को समझने में समय लगना स्वाभाविक है । इस विषय में हम आगे विस्तारपूर्वक लिखेंगे । अभी यह लिखना पर्याप्त है कि स्वामीजी के जीवन का एक महान् कार्य वेदभाष्य करना भी था ।
स्वामी दयानन्द के जीवन का तृतीय महान् कार्य वेदभाष्य करना था
स्वामी दयानन्द ने अपनी दूरदर्षिता से यह समझ लिया था कि हिन्दू धर्म का सुधार किसी एक व्यक्ति के द्वारा सम्भव नहीं है और न यह थोड़े समय में ही हो सकता है । इसे यों भी कहा जा सकता है कि वैदिक धर्म का पुनरुद्धार एक ऐसा कार्य है जो एक व्यक्ति के द्वारा एक जीवन में किया जाना सम्भव नहीं है । इसलिये उन्होंने यह जरूरी समझा कि एक ऐसा संगठन बने जो उनके द्वारा उठाये गये कार्य को करता रहे । यह संस्था ईश्वर की निराकारोपासना का प्रचार करेगी, मूर्तिपूजा का खण्डन करेगी और उसे वेदविरुद्ध सिद्ध करती रहेगी । वह वेदों के अर्थ करने में प्राचीन ग्रन्थों की सहायता लेगी ।
स्वामीजी हिन्दू परिवार में जन्मे, वहीं उनका पालन हुआ, उन्हें के शास्त्रों को पढ़ा तथा इस धर्म के पवित्र ग्रन्थों को अपना मार्गदर्शक माना । आर्यों की आश्रम-व्यवस्था को उन्होंने स्वीकार किया था । अतः यह स्वाभाविक ही था कि उनके हृदय में हिन्दू जाति के सुधार का भाव आता । आर्यों के पवित्र पुरातन धर्म को जान कर उस धार्मिक पुरुष के मन में यह विचार आया कि धर्म-सुधार के बिना इस जाति का सुधार असम्भव है । उन्होंने अपने जीवन का बहुमूल्य भाग सच्चे धर्म की खोज में व्यतीत किया । यह सम्भव ही नहीं था कि वे धर्म के अतिरिक्त अन्य किसी विषय को अपने सुधार का विषय बनाते । उनके जैसे महापुरुष के लिये यह समझ लेना स्वाभाविक ही था कि धार्मिक सुधार के बिना इस धर्मभूमि भारत का सुधार असम्भव ही है । अतः सुधार के इस विचार को ही प्रधानता देकर उन्होंने एक ऐसी संस्था का बीजारोपण किया जिसका उद्देश्य था - देश में धर्म-सुधार करना तथा सच्चे वेदाधारित धर्म का प्रचार करना ।
तथापि यह याद रखना आवश्यक है कि स्वामीजी का विचार किसी नये सम्प्रदाय या मत की नींव डालना कदापि नहीं था । अपितु उनका विचार तो पुरातन शुष्क धर्मवृक्ष को हराभरा करने का ही था । उसे पुनरुज्जीवित करना था । वे सुधार का कार्य करना चाहते थे न कि अराजकता उत्पन्न करने वाली कोई क्रान्ति । इसलिये उन्होंने अपने द्वारा स्थापित समाज के कोई नये सिद्धान्त नहीं बनाये । दो मन्तव्यों पर उनका दृढ़ विश्वास था - (1) प्रथम तो यह कि जो विद्या या पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका आदिमूल परमेश्वर है और इस विद्या का ज्ञान पुरुषों को परमात्मा से वेदों के द्वारा ही मिला है । (2) यह कि परमात्मा निराकार और अजन्मा है तथा उसकी उपासना करना ही हमारा परम धर्म है । ये दोनों नियम उनके जीवनाधार थे और इन सिद्धान्तों को स्वीकार किये बिना किसी प्रकार का सुधार सम्भव नहीं था । वे यह भी जानते थे कि यदि हिन्दू धर्म में एकता स्थापित हो सकती है तो इन्हीं दो सिद्धान्तों के सहारे । इन्हें त्याग कर जातीय एकता कदापि सम्भव नहीं है । अतः उन्होंने आर्यों की धार्मिक एकता के लिये इन दो सिद्धान्तों को नींव का पत्थर बनाया ।
सर्वप्रथम आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुई । उस समय आर्यसमाज के जो नियम बनाये गये उनमें उपर्युक्त दोनों धार्मिक नियम थे । उसके बाद लाहौर में इन नियमों का पुनरवलोकन किया गया और आर्यसमाज के सार्वकालिक नियमों से भिन्न उपनियम भी बनाये गये । उस समय भी परमात्मा और वेद विषयक मन्तव्यों पर विशेष ध्यान दिया गया तथा इनके लिये तीन नियम बने । आर्यसमाज के ये प्रथम तीन नियम ही वास्तव में उसके प्रमुख धर्म सिद्धान्त हैं ।
वेदों के विषय में स्वामीजी का विश्वास उनके द्वारा रचित ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका तथा सत्यार्थप्रकाश में वर्णित है । वे चारों वेदों को ईश्वरकृत मानते हैं और किसी मनुष्य को इस विषय में संदेह करने की आज्ञा नहीं देते । तथापि आर्यसमाज के नियम बनाते समय उन्होंने अपने शब्दों का प्रयोग न कर प्राचीन शास्त्रकारों के शब्दों को ही ग्रहण किया । बम्बई में बनाये गये नियमों में यह शब्द थे - “इस समाज में मुख्य स्वतःप्रमाण वेदों का ही प्रमाण माना जाएगा” और लाहौर में निर्मित नियम इस प्रकार हैं - “वेद सब विद्याओं का सत्य पुस्तक है ।” दोनों वाक्य शास्त्रकारों के हैं । समस्त शास्त्रकार वेदों को स्वतःप्रमाण मानते हैं । वेदों की सिद्धि के लिए किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं रहती । बम्बई के नियमों में ‘मुख्य’ शब्द इसलिये था कि उससे वेदों के तथा प्रकृति के नियमों का भेद किया जा सके । प्रकृति नियम भी स्वतःप्रमाण होते हैं परन्तु उनको समझने के लिये विद्या की आवश्यकता होती है जो वेदों से ही प्राप्त हो सकती है । इसलिये वेद ही मुख्य स्वतःप्रमाण सिद्ध हुए परन्तु लाहौर में और भी सरल शब्दों के प्रयोग की आवश्यकता समझी गई इसलिये ‘स्वतःप्रमाण’ इस संस्कृत शब्द को छोड़कर ‘सत्य विद्याओं का पुस्तक’यह वाक्यांश रखा गया । वेदों के विषय में स्वामीजी ने उन शब्दों का प्रयोग उचित समझा जिसके सम्बन्ध में समस्त आर्य शास्त्रकार एकमत थे । बौद्धों को छोड़कर कोई भी आर्य शास्त्रकार ऐसा नहीं जो वेदों को इतना उच्च स्थान न देता हो, जो आर्य समाज के तीसरे नियम में दिया गया है । स्वामीजी उसी धर्म का प्रतिपादन करते थे जिसके विषय में शास्त्रकारों की एक सम्मति थी । किसी नवीन मत को स्थापित करना उनका उद्देश्य नहीं था । अनेक स्थानों पर लोगों ने उनसे कहा कि यदि वे तीसरे वेद विषयक नियम को हटा दें तो बहुत से मनुष्य आर्यसमाज में प्रविष्ट हो जायेंगे । किन्तु उन्होंने इसे कभी स्वीकार नहीं किया । वेदों के बिना वे किसी धर्म की कल्पना भी नहीं कर सकते थे और न वेदों से भिन्न किसी अन्य धर्म को मानते थे । वेदों पर वे दृढ़ता से जमे हुए थे । ब्रह्मसमाज और आर्यसमाज को एक करना उनके जीवन का उद्देश्य नहीं था । उनके जीवन का ध्येय था वेदों को आर्य जाति का मुख्य आश्रय बनाना तथा वेदों को धर्म का आदि स्रोत सिद्ध करना । यदि वे इस विषय में आग्रह नहीं रखते तो उन्हें वह उच्च पद प्राप्त नहीं होता जो आर्य जाति में प्राप्त हुआ है । वेदों के अभाव में हिन्दू धर्म का जीवित रहना ही कठिन है । ईश्वरीय ज्ञान के बिना धर्म निर्मूल है । ईश्वरीय शिक्षा के अभाव में धर्म अंधा और लंगड़ा है । ईश्वरीय ज्ञान के बिना धर्म पंगु होता है । अनेक आर्यसमाजियों ने भी स्वामीजी से विनय की कि वे तीसरे नियम के शब्द ही बदल दें जिससे वेदों का वह महत्त्व न रहे जो आज है, किन्तु इसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया । इस तथ्य से ही स्वामी दयानन्द का महापुरुषत्व सिद्ध होता है ।
आर्यसमाज की स्थापना स्वामी दयानन्द का चौथा महत्वपूर्ण काम था
स्वामीजी की दृष्टि में आर्यसमाज का क्या उद्देश्य था ?
क्या स्वामी दयानन्द की दृष्टि में एक ईश्वर की उपासना का प्रचार करना और वेदों को सत्य विद्या का पुस्तक सिद्ध करना ही आर्यसमाज का काम था या इससे भिन्न भी वे इसका कोई उद्देश्य मानते थे ? आर्यसमाज के शेष नियम इस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं हैं यद्यपि छठा नियम यह कहता है कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात् शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना । परन्तु इन शब्दों से यह नहीं समझना चाहिए कि स्वामीजी के कार्यक्रम में देश या जाति की उन्नति के लिये कोई स्थान नहीं था । १ अप्रैल १८७८ को दानापुर से लिखे एक पत्र में उन्होंने लिखा -
- “आपकी इच्छानुसार कल 31 मार्च 1878 को दो छपे पत्र (आर्यसमाज के मुख्य दस उद्देश्य) भेज चुके हैं । रसीद शीघ्र भेज दीजिये और इन नियमों को ठीक-ठीक समझ कर वेद की आज्ञानुसार देश को सुधारने में अत्यन्त श्रद्धा, प्रेम और भक्ति, सबके परस्पर सुख के अर्थ तथा उनके क्लेशों को मेटने में सत व्यवहार और उत्कण्ठा के साथ अपने शरीर के सुख-दुखों के समान जान कर सर्वदा यत्न और उपाय करने चाहियें । क्योंकि इस देश से विद्या और सुख सारे भूगोल में फैला है । हिन्दू मत सभा के स्थान में आर्यसमाज नाम रखना चाहिए क्योंकि आर्य नाम हमारा और आर्यावर्त नाम हमारे देश का सनातन वेदोक्त है ।”
फिर 12 अप्रैल 1878 के पत्र में लिखते हैं - “अब आपकी दृष्टि देश सुधार पर होनी चाहिए ।” याद रखना चाहिए कि आर्यसमाज के दस नियम जून 1877 में नियत किये गये थे और ये पत्र अप्रैल 1878 में लिखे गये हैं । स्वामीजी की दृष्टि में आर्यसमाज का क्या उद्देश्य था, वह इन पत्रों से प्रकट होता है । क्या इन पत्रों से यह विदित नहीं होता कि स्वामीजी उन लोगों में नहीं थे जो मनुष्य मात्र के हित की तुलना में अपने देश और जाति का कोई स्वत्व नहीं मानते ? वास्तव में बात यह है कि स्वामीजी पहले संस्कृत विद्वान थे जिन्होंने स्वार्थ के जाल में फँसे हिन्दुओं को बताया कि परोपकार और देशोपकार धर्म के दो प्रमुख अंग हैं और वैदिक धर्म में इन्हें बहुत ऊँचा स्थान प्राप्त है । जो मनुष्य परोपकार और देशोपकार नहीं कर सकते वे कभी धार्मिक भी नहीं हो सकते और देश के उपकार को जीवन का प्रथम ध्येय न मानने वाला भी कभी धार्मिक नहीं हो सकता ।
बम्बई में जो नियम बनाये गये थे उनमें नियम 17 अपनी व्याख्या स्वयं ही करता है -
- “इस समाज में स्वदेश के हितार्थ दो प्रकार की शुद्धि के लिये प्रयत्न किया जाएगा । एक परमार्थ और दूसरा लोक-व्यवहार । इन दोनों का शोधन और शुद्धता की उन्नति तथा सब संसार के हित की उन्नति की जाएगी ।”
बम्बई के नियम यह भी बताते हैं कि स्वामीजी की सम्मति में आर्यसमाज के उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधन क्या थे । 12वें नियम में आर्यसमाज, आर्य विद्यालय और आर्य प्रकाश (पत्र) के प्रचार और उन्नति के लिये 1 रुपया सैंकड़ा चंदा लेने की शिक्षा है । यहाँ आर्यसमाज से आशय प्रचार और संगठन के खर्च से है । 19वें नियम में प्रचारक भेजने की बात आई है । 20वें में स्त्रियों और पुरुषों के लिये पाठशालायें नियत करने की आवश्यकता बताई गई है । लाहौर में बने तीसरे नियम में कहा है - “वेदों का पढ़ना-पढ़ाना, सुनना-सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है ।” साथ ही आठवें में अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करने की आज्ञा है ।
इसके अतिरिक्त दिल्ली के शाही दरबार के अवसर पर स्वामीजी की प्रेरणा से जो एक सम्मेलन अयोजित किया गया था वह भी उनकी देशभक्ति का परिचय देता है (द्रष्टव्य - पं० लेखराम कृत उर्दू जीवनचरित, पृ० २६४) । स्वामीजी ने वहाँ कहा था - “यदि हम लोग एकमत हो जायें और एक ही रीति से देश का सुधार करें तो आशा है देश शीघ्र सुधर सकता है ।”
इस जीवनचरित में यह भी लिखा है कि एक स्थान पर स्वामीजी ने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर एक विशेष व्याख्यान दिया । इन सब तथ्यों से स्वामीजी का देशभक्त होना स्वतः ही सिद्ध हो जाता है । वस्तुतः वे तो देशभक्त महापुरुषों में भी शीर्ष स्थान पर बिठाने जाने की योग्यता रखते हैं । ऐसे लोग संसार में बहुत कम पैदा होते हैं जो देश और जाति के लिए प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं । ऐसे मनुष्यों का कोई भी कार्यक्रम स्वदेश और स्वजाति के हित से रहित नहीं हो सकता । अतः हम निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि देश और जाति के सुधार की एक सुनिश्चित योजना स्वामी दयानन्द के पास थी ।
स्वामी दयानन्द के अन्य सिद्धान्त
हमने ऊपर स्वामीजी के पत्रव्यवहार से ही उनके महान् कार्यों और उद्देश्यों का वर्णन किया है । परन्तु उन्होंने अपने अल्पकालीन जीवन में अन्य भी अनेक महत्त्वपूर्ण शिक्षायें दी हैं । उनके जैसे सुधारक के लिये यह सम्भव नहीं था कि वे केवल महत्त्वपूर्ण विषयों की ही चर्चा करते और अन्य गौण विषयों को छोड़ देते । उन्होंने जहाँ प्रचलित धर्म और रीति-नीति की आलोचना की है वहीं अनेक विधेयात्मक उपदेश भी दिये हैं ।
- श्राद्ध, तीर्थ और अवतार
- धार्मिक विषयों में उन्होंने केवल मूर्तिपूजा पर ही आक्रमण नहीं किया अपितु प्रचलित श्राद्ध प्रणाली, तीर्थ और अवतारवाद का भी खण्डन किया । उन्होंने बताया कि मृत पितरों के नाम पर दान देने से उनकी आत्मा को कोई लाभ नहीं पहुँचता । किसी जलाशय तथा नदी में स्नान करने से पापों का विनाश नहीं होता और मुक्ति भी नहीं मिलती । परमात्मा अजन्मा और अमर होने से कभी मनुष्य देह में नहीं आता ।
- नवीन वेदान्त
- उन्होंने नवीन वेदान्त की शिक्षा का भी खण्डन किया और बतलाया कि आत्मा और परमात्मा दो पृथक् पदार्थ हैं तथा प्रकृति भी अनादि है । तथापि परमात्मा सर्वशक्तिमान् और सृष्टि का आदि कारण है ।
- मुक्ति
- इस विषय में उनका कहना है कि जीव मुक्त होकर परमात्मा के सानिध्य में निश्चित अवधि तक दिव्यानन्द का भोग करता है, तत्पश्चात् पुनः संसार में आता है ।
- आवागमन
- स्वामीजी कर्म-सिद्धान्त को मानते थे । उनका यह मन्तव्य था कि आत्मा बार-बार जन्म लेता है और भिन्न-भिन्न योनियों में कर्म करते हुए फल भी भोगता है । पवित्र और शुद्ध आत्मा मोक्ष को प्राप्त करता है तथा निश्चित समय के लिये जन्म-मरण के बंधन से छूट जाता है ।
- शिक्षा
- इस विषय में उनकी सम्मति थी कि प्रत्येक वर्ण के बालक और बालिका को विद्या ग्रहण करनी चाहिए तथा इसका अधिकार सभी को है ।
- सामाजिक व्यवहार
- स्वामीजी बाल-विवाह के विरोधी थे और इसको शारीरिक निर्बलता का कारण मानते थे । उनकी सम्मति में पुरुष के लिए 25 वर्ष तक तथा कन्या के लिये 16 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन आवश्यक है । विवाह में वर और कन्या की सहमति को जरूरी समझते थे । इसलिये वे अक्षतवीर्य युवा-युवतियों के विवाह के समर्थक थे । द्विजों में पुनर्विवाह को अच्छा नहीं मानते थे किन्तु सन्तानोत्पत्ति के लिये नियोग की आज्ञा देते थे ।
- जाति और संस्कार
- जाति (वर्ण) को जन्माधारित नहीं वरन् कर्म के अनुसार मानते थे । प्रत्येक आर्य के लिए शिखा और यज्ञोपवीत को आवश्यक बताते थे । प्रत्येक स्त्री-पुरुष के लिए सोलह संस्कारों को अनिवार्य मानते थे । भोजन-व्यवहार में आर्येतर लोगों के हाथ का खान-पान उचित नहीं समझते थे । मदिरापान और मांस-भक्षण को भी अनुचित मानते थे । उनके जीवन की एक घटना इस प्रकार है । “तब जोन्स साहब ने कहा, ...तो आप छूतछात को क्यों मानते हैं, हमारे साथ खाने में क्या डर है ? उत्तर दिया कि किसी के साथ खाने या न खाने में हम धर्म या अधर्म नहीं मानते । यह सब देश और जाति के रिवाजों से सम्बन्धित है । वास्तविक धर्म से इसका कुछ सम्बन्ध नहीं है । जो समझदार हैं वे अकारण ही देशाचार के विरुद्ध काम नहीं करते । क्या आप अपने पुत्र का विवाह किसी देसी ईसाई से कर सकते हैं ?” आदि । यह भी वर्णित हुआ है कि देहरादून में उन्होंने एक ब्रह्मसमाजी के घर बना भोजन खाने से मना कर दिया था क्योंकि वह भंगिन के हाथ का बना हुआ था ।
क्या स्वामी दयानन्द सिद्ध थे ?
हम यह तो स्वीकार करते हैं कि स्वामीजी बड़े भारी योगी थे किन्तु जो लोग उन्हें सिद्ध प्रमाणित करने का यत्न करते हैं हम उनका खण्डन करते हैं । स्वामीजी ईश्वर-प्राप्ति के लिये योग विद्या को जरूरी समझते हैं । परन्तु उन्होंने अपने समस्त जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे लोगों को यह बतलायें कि वे योग बल से भविष्य के हालात जान लेत हैं, किसी के मन की बात को समझ लेते हैं अथवा किसी गुम हुई वस्तु अथवा व्यक्ति का पता बता सकते हैं । उन्हें भविष्यवक्ता कहलाने जैसा कोई काम नहीं किया और जो उन्हें ऐसा कहता है हम उसे अस्वीकार करते हैं । उनके ग्रन्थों में इस बात की गंध तक नहीं है । अच्छा हो ऐसे लोग उनकी इस प्रकार श्लाघा कर उन्हें बदनाम न करें । इसके विपरीत कर्नल आल्काट और मैडम ब्लैवेट्स्की से हुए उनके पत्र-व्यवहार से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि वे इस प्रकार के चमत्कारों को दिखाने के विरोधी थे । ऐसे खेल तो थियोसोफिकल सोसाइटी के सदस्य अपने कथित योग विद्या के प्रदर्शन के लिये दिखलाया करते हैं ।
स्वामी दयानन्द और शुद्धि
स्वामीजी द्वारा किये गये शुद्धि कार्य के वर्णन के बिना उनके जीवन का यह विवेचन अधूरा रहेगा । यह काम शुद्धि का था । गुरु गोविन्दसिंह के बाद स्वामी दयानन्द ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिन्दुओं को शुद्धि के लिये प्रेरित किया । स्वामीजी के कार्यक्षेत्र में आने से पहले विदेशों से लौटे हिन्दुओं को पुनः शुद्ध करने और प्रायश्चित्तपूर्वक समाज में सम्मिलित करने पर विवाद था । सर्वसाधारण पण्डित हिन्दुओं का समुद्र पार जाना ही अनुचित समझते थे । उनके धर्मशास्त्र कहते थे कि विदेश से लौटा हिन्दू पुनः अपनी जाति में प्रविष्ट नहीं हो सकता । अन्य विद्वानों का कहना था कि हमारे प्राचीन सूत्र तथा स्मृति ग्रन्थ इस बात की आज्ञा देते हैं कि आवश्यकतानुसार यदि आर्य लोग समुद्र यात्रा करें तो लौटने पर प्रायश्चितपूर्वक शुद्ध हो जाएँ । किन्तु उस समय कोई स्वप्न में भी नहीं सोचता था कि धर्म से पतित हिन्दू से मुसलमान या ईसाई बनने के बाद भी वह स्वजाति या स्वधर्म में प्रवेश पा सकता है । स्वामी दयानन्द ने ऐसा पंजाब के जालंधर नगर में किया जहाँ एक ईसाई बने बालक को उन्होंने पुनः उसकी जाति में प्रविष्ट करा दिया । (द्रष्टव्य - पं० लेखराम रचित जीवनचरित, पृष्ठ 333) अमृतसर में शुद्धि पर व्याख्यान दिया । देहरादून में एक जन्मना मुसलमान को आर्यसमाज में मिला लिया । लाहौर और अन्यत्र अंग्रेजों, ईसाइयों तथा मुसलमानों के पूछने पर कहा कि आर्यों जैसा आचरण कर आप भी आर्य बन सकते हैं । इस समय पंजाब में शुद्धि का जो कार्य हो रहा है वह उनकी शिक्षा का ही फल है । उनके पहले किसी भी हिन्दू या सिख का यह साहस नहीं था कि वह अपने धर्म से पतित किसी स्त्री-पुरुष को पुनः अपने में मिला ले । स्वामीजी ने शुद्धि का उपदेश देकर हिन्दू जाति को बचाया और जाति की डूबती नौका को उबार लिया । सैंकड़ों परिवारों को विनाश से बचाया, सहस्रों बालकों को अनाथ होने से बचाया तथा हजारों स्त्रियों को वैधव्य की पीड़ा से सुरक्षित किया ।
स्वामी दयानन्द और अनाथ रक्षा
स्वामीजी को अपने देश के अनाथ बालकों की रक्षा का पूरा ध्यान था । उन्होंने अपने जीवनकाल में फीरोजपुर के अनाथालय की स्थापना की । वे खुद परोपकार के इस कार्य में सहायक थे । अपने स्वीकार-पत्र में अपनी स्थानापन्न परोपकारिणी सभा के उद्देश्यों में भी उन्होंने अनाथ रक्षा को प्रमुख रखा और कहा कि आर्यावर्त के दीन-अनाथों के पालन एवं शिक्षण में इस सभा का धन व्यय किया जाएगा ।
स्वामीजी के हृदय में जाति रक्षा का विचार कूट-कूट कर भरा हुआ था । उनके आचरण और कार्यों से विदित होता है कि अनाथों की रक्षा के प्रति हिन्दू समाज की विरक्ति को वे अपने संवेदनायुक्त तथा प्रेमपूर्ण हृदय में कैसा अनुभव करते थे । भिखारी रूपी तीर्थ-पण्डों ने अपने दान-दक्षिणा इतनी बढ़ा दी थी कि दान का वास्तविक रूप ही लुप्त हो गया था । फलतः लाखों अनाथ बालक अन्य धर्मों में प्रविष्ठ हो जाते थे । अन्य मतावलम्बियों ने तो अनाथालयों की स्थापना करके ऐसे अनाथ बालकों को अपनी ओर खींचने की व्यवस्था कर रखी थी । स्वामीजी भी इस कार्य के महत्त्व को जानते थे । इसे अनुभव कर उन्होंने आर्यसमाज में भी अनाथों के पालन तथा रक्षा के लिये विशेष प्रावधान करने पर जोर दिया । हमें यह सुन कर दुःख होता है जब कई लोग कहते हैं अपने वसीयतनामे में स्वामीजी ने अनाथ पालन को तीसरे स्थान पर रखा है और इसका अर्थ वे यह करते हैं कि जब पहले बताये दोनों कर्त्तव्य पूरे हो जाएँ तब इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए । हमें इस विचार को सुनकर ही लज्जा और हँसी आती है । हँसी उन लोगों की बुद्धि पर आती है जो स्वीकार-पत्र की ऐसी व्याख्या करते हैं । लज्जा इसलिए कि जिन लोगों को स्वामीजी के उपदेशों को सुनने का अवसर मिला था वे भी उस महापुरुष के कहे स्पष्ट वाक्यों की कैसी गलत व्याख्या करते हैं । हमारे विचार से इस विचित्र व्याख्या की चर्चा करना भी व्यर्थ है । हमने स्वामीजी के स्वीकार-पत्र को इस ग्रन्थ के अन्त में दिया है, उसे पढ़ कर आप स्वयं विचार कर सकते हैं ।
अन्तिम निवेदन
पाठक महाशय, हमारी भूमिका बहुत बढ़ गई है और आप इसके और अधिक विस्तार से घबरा न जायें । इसलिए अब हम उन महापुरुष के जीवन-वृत्तान्त को प्रस्तुत करते हैं जिनके कार्यों की संक्षिप्त समालोचना हमने भूमिका में संक्षेप में की है । जो हमें अधिक कहना है वह आगे के पृष्ठों में कहेंगे । हमें विश्वास है कि पक्षपातरहित होकर यदि इसे पढ़ेंगे तो आप इस बात से अवश्य सहमत हो जाएँगे कि स्वामीजी एक महापुरुष थे, चाहे आपके धार्मिक विचार स्वामीजी के विचारों के अनुरूप हों या न हों । आप यह भी स्वीकार करेंगे कि आर्य जाति उन पर जितना भी गर्व करे, वह कम है ।
एक बात हम अपने युवकों से कहना चाहते हैं । हमारी जाति के होनहार बालको, स्वामीजी को आपके हित की विशेष चिन्ता थी । वे जहां जाते थे, विद्यार्थी उन्हें चारों ओर से घेर लेते थे । वे उन पर प्राण देते थे और विद्यार्थी भी उन पर न्यौछावर थे । वे समझते थे कि ये विद्यार्थी ही हमारे देश और जाति की आशा हैं, इन पर ही देश की उन्नति और प्रतिष्ठा निर्भर है । विद्यार्थी भी जानते थे कि वह पुरुष हमारा शुभचिन्तक है । इन्होंने ही हमें अपनी जाति और साहित्य का मान करना सिखाया है । नवयुवकों के लिये यह पुस्तक बहुमूल्य उपदेशों से भरी हुई है । हमें पूरा विश्वास है कि हमारी जाति के युवा उस महापुरुष के जीवन से पूर्ण लाभ उठा कर उनकी आज्ञा का पालन करेंगे । नौजवानो , आओ । हम तुमको उस जितेन्द्रिय, बाल ब्रह्मचारी, महोपकारी, देश-हितैषी, विद्वान्, योगी महर्षि दयानन्द के जीवन की कथा सुनाते हैं । परमात्मा से प्रार्थना करो कि वह इस जीवनचरित से यथायोग्य लाभ उठाने के लिये तुम्हारी बुद्धि को निर्मल और पवित्र बनाये । ओ३म् शान्ति शान्ति शान्ति ।
- लाजपतराय
1857 के संग्राम में स्वामी दयानन्द का योगदान
स्वामी दयानन्द क्रान्ति की इस योजना से पूरी तरह परिचित थे। सन् 1856 ई० के मई मास में स्वामी दयानन्द नाना साहब के घर कानपुर गये और 5 मास तक कानपुर और इलाहाबाद के बीच ही चक्कर काटते रहे। (“सन् 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम में स्वराज्य प्रवर्तक महर्षि दयानन्द सरस्वती का क्रियात्मक योगदान”, ग्रन्थलेखक स्वामी गिरीराज ने, पृ० 12 पर यह सब स्पष्ट सप्रमाण प्रस्तुत किए हैं)।
संवत् 1913 वि० (सन् 1856 ई०) में कुम्भ मेले के अवसर पर स्वामी दयानन्द हरद्वार पहुंचे
जाट वीरों का इतिहास: दलीप सिंह अहलावत, पृष्ठान्त-603
थे। स्वामी जी ने नील पर्वत पर चण्डी मन्दिर को अपना निवास स्थान बनाया। चण्डी स्थान के संन्यासी स्वामी रुद्रानन्द जी ने आपको बताया कि “भारतवासी प्रजा-जागरण और विप्लव प्रचेष्टा के नायक नेता यहां चण्डी पर्वत पर आने वाले हैं।” तीन दिन के पश्चात् ही पांच अज्ञात सज्जन वहां पधारे। उन्होंने पूछा महात्मा स्वामी दयानन्द जी कहाँ हैं? साक्षात्कार होने पर स्वामी दयानन्द ने उनका परिचय पूछा। इस पर उन्होंने बताया कि वे हैं - 1. द्वितीय बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र धुन्धुपन्त (नाना साहब पेशवा) 2. श्री बाला साहब 3. श्री अजीमुल्ला खां। 4. श्री तांत्या टोपे 5. जगदीशपुर के राजा कुंवरसिंह। एकान्त स्थान में बैठकर स्वामीजी ने इनके साथ क्रान्ति के विषय में बहुत देर तक बातचीत की। इस बैठक में स्वामीजी ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए साधुसमाज के अन्दर क्रान्ति करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया, क्योंकि इन पांचों ने ही स्वामी जी से साधु संगठन के लिए अनुरोध किया था। उन्होंने कहा था, “महाराज! प्रजा विद्रोह के कार्य में पेशावर से कलकत्ता और मेरठ से कर्नाटक तक सहस्रों भारतीय नियुक्त हो चुके हैं, परन्तु संगठन का कार्य अभी तक अधूरा ही पड़ा है, आप कृपया इसे पूर्णतः सफल कीजिए।”
उपर्युक्त पांच क्रान्तिदूतों के अतिरिक्त दो अन्य क्रान्तिकारी स्वामी दयानन्द जी से भेंट के लिए पधारे थे। वे थे राजा गोविन्दराय और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई।
राजा गोविन्दनाथ राय - यह उत्तरीय बंगाल में नादौर की प्रसिद्ध रानी भवानी के वंशज थे। अंग्रेजों ने उनका सारा राज्य हड़प लिया था। आपने चण्डी पर्वत पर स्वामी दयानन्द से अपने राज्य सम्बन्धी तथा योग विषयक चर्चाएं कीं। राजा साहब ने स्वामी जी को 1101 रुपये भेंट के रूप में प्रस्तुत किए। स्वामी जी ने बहुत कहा कि “मुझे इस धन की आवश्यकता नहीं है।” परन्तु वह नहीं माने और सादर नमस्कार करके चले गए।
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई - इनके दो-तीन दिन बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपनी सपत्नी रानी गंगाबाई और तीन कर्मचारियों सहित स्वामी जी से मिली। स्वामी जी ने उनका परिचय पूछा। इस पर आंसूभरे नयनों से रानी ने ओजपूर्ण भाषा में कहा - “महाराज! मैं एक निःसन्तान विधवा हूँ। इसी बहाने से अंग्रेजों ने मेरे झांसी के राज्य पर अधिकार कर लेने की घोषणा कर दी है। ये एक विशाल सेना लेकर मेरी झांसी पर चढ़ाई करने वाले हैं। परन्तु मैं जीवित रहती हुई अपने श्वसुर कुल का राज्य इन्हें हड़पने न दूंगी। आप आशीर्वाद दें कि मैं वीरांगनाओं की भांति लड़ती-लड़ती स्वदेश पर बलिदान हो जाऊं।”
इस वीर रमणी के मुख से ऐसे उद्गार सुनकर स्वामी जी ने प्रसन्न होकर कहा - “देवि! यह शरीर क्षणभंगुर और नाशवान् है। यह सदैव नहीं रह सकता। धन्य हैं वे व्यक्ति जो धर्म पर इसे न्यौछावर कर देते हैं। वे मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। अतः तलवार उठाओ और इन फिरंगियों के साथ साहस से युद्ध करो।”
उक्त रानी ने भी 1101 रुपये स्वामी जी को भेंट किए। स्वामी जी ने उसे भी कहा कि “मेरे को धनराशि की आवश्यकता नहीं है”, पर वह न मानी और नमस्कार करके चली गई।
रानी लक्ष्मीबाई के चले जाने के 7-8 दिन बाद फिर नाना साहब पेशवा आदि स्वामी जी को सारा
जाट वीरों का इतिहास: दलीप सिंह अहलावत, पृष्ठान्त-604
समाचार देने के लिए पधारे। स्वामी जी ने नाना साहब को, गोविन्दनाथ राय वाले 1101 रुपये, रानी झांसी वाले 1101 रुपये तथा जनसाधारण के मिले 633 रुपये, कुल 2835 रुपये स्वदेश रक्षार्थ दे दिए। स्वामी जी ने नाना साहब को कहा कि “जन साधारण का नेतृत्व करना और लेकर खेलना दोनों ही खतरनाक हैं। मामूली-सी भूल से ही सत्यानाश हो सकता है। अतः संभलकर सारा काम करो। गुप्त रीति से क्रांति की सूचना सारे देश में भेज दें।” स्वामी जी ने भी पूर्ण शक्ति से साधु संगठन का काम आरम्भ कर दिया। (हरयाणा सर्वखाप पंचायत रिकार्ड)
सन् 1857 से 1860 तक तीन वर्ष का स्वामी दयानन्द के जीवन का कोई इतिवृत्त नहीं मिलता। इससे द्योतित होता है कि स्वामी जी ने 1857 ई० की क्रान्ति में बढ़-चढ़कर कार्य किया और अपने हस्तलिखित जीवन में भी इस सम्बन्ध में उन्होंने कुछ लिखना और किसी कारणवश उचित नहीं समझा। अक्टूबर सन् 1860 ई० के पश्चात् स्वामी दयानन्द की जीवन घटनायें विदित होती हैं। स्वामी दयानन्द ने सन् 1860 से 1863 तक तीन वर्ष स्वामी विरजानन्द जी से विद्याध्ययन किया। (सुधारक बलिदान विशेषांक, पृ० 468, लेखक भगवान् देव आचार्य।
स्वामी दयानन्द धार्मिक महर्षि के अतिरिक्त देशभक्त एवं स्वतन्त्रता प्राप्ति के कार्यकर्त्ता भी थे। उन्होंने अपने पुस्तक सत्यार्थप्रकाश के अष्टम समुल्लास में लिखा है कि “कोई कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है अथवा मतमतान्तर के आग्रह रहित, अपने और पराये का पक्षपातशून्य, प्रजा पर माता-पिता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है।”[1]
सत्यार्थप्रकाशः क्यों पढ़ें ?
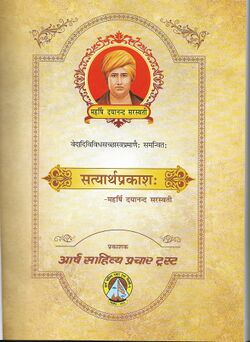
- जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त (तक) मानव जीवन की लौकिक - परालौकिक समस्त समस्याओं को सुलझाने के लिए यह ग्रन्थ एकमात्र अमूल्य ज्ञान का भण्डार है ।
- इस ग्रन्थ में प्रतिपादित सर्वतंत्र, सार्वजनीन, सनातन मान्यताओं के परीक्षण के लिए आह्वान किया गया है।
- इस ग्रन्थ में ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यन्त ऋषि मुनियों के वेद प्रतिपादित सारभूत विचारों का संग्रह है ।
- अल्पविद्यायुक्त स्वार्थी, दुराग्रही लोगों ने जो वेदादि सत्य शास्त्रों के मिथ्या अर्थ करके उन्हें कलंकित करने का दुःसाहस किया था, उनके मिथ्या अर्थों का खण्डन और सत्यार्थ (सत्य सत्य अर्थों) का प्रकाश अकाट्य युक्तियों और प्रमाणों से इस ग्रन्थ में किया गया है | किसी नवीन मत की कल्पना इस ग्रन्थ में लेशमात्र भी नहीं है ।
- वेदादि सत्य शास्त्रों के अध्ययन के बिना सत्य ज्ञान की प्राप्ति सम्भव नहीं | उनको समझने के लिए यह ग्रन्थ कुञ्जी का काम करता है | इस ग्रन्थ के अध्ययन करने से वेदादि सत्य शास्त्रों का सत्य - सत्य अर्थ समझना सरल हो जाता है ।
- अत्यन्त समृद्धिशाली, सर्वदेश शिरोमणि भारत देश का पतन किस कारण से हुआ एवं पुनः उत्थान कैसे हो सकता है, इस विषय पर पूर्ण प्रकाश डाला गया है।
- मानव जाति के पतन का कारण जो मतवादियों की मिथ्या धारणाएँ हैं, उनका पूर्णतया निष्पक्ष, सप्रमाण और युक्तिपूर्ण खण्डन इसमें किया गया है |
- इसमें मूल दार्शनिक सिद्धान्तों को ऐसी सरल रीति से समझाया गया है कि इसे पढ़कर साधारण शिक्षित व्यक्ति भी एक अच्छा दार्शनिक बन सकता है । जिस ने इस ग्रन्थ को न पढ़कर नव्य (नये) महाकाव्य अनार्ष ग्रन्थों के आधार पर दार्शनिक सिद्धान्तों को पढ़ा है, उस की मिथ्या धारणाओं का खण्डन और सत्य मान्यताओं का मण्डन इस ग्रन्थ का अध्ययन करने वाला कर सकता है।
- ऋषि मन्तव्यों पर इस ग्रन्थ को पढ़ने से पूर्व जितनी भी शंकाएं किसी को होती हैं, वे सब इस के पढ़ने से समूल नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि उन सब शंकाओं का समाधान इसमें विद्यमान है।
- धर्म के मौलिक और वास्तविक स्वरूप का पूर्ण परिचय केवल इस ग्रन्थ में मिलता है ।
- इसकी एक विशेषता यह भी है कि अध्याय शब्द के स्थान पर समुल्लास शब्द का प्रयोग किया गया है, जो दो शब्द (सम् + उल्लास = समुल्लास) का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है (सम्) यानि समान और (उल्लास) यानि प्रसन्नता | इनको मिलाने पर समुल्लास का अर्थ हुआ समान प्रसन्नतापूर्ण । अर्थात् सत्यार्थप्रकाश में सभी समुल्लासों को लिखते समय एक जैसा प्रसन्न भाव रखा गया है । किसी भी विषय की व्याख्या करने, खण्डन-मण्डन करने अथवा समीक्षा करने में एक जैसा प्रसन्न भाव रखा गया है। लेशमात्र भी कहीं कोई नाराजगी, द्वेष, ईर्ष्या, अन्यथा भाव या पूर्वाग्रह युक्त होकर इस ग्रन्थ को नहीं लिखा गया है ।
- ऋषि दयानन्द से पूर्ववर्ती ऋषियों के काल में संस्कृत की व्यापक रूप में व्यवहार था और वेदों के सत्य अर्थ का ही प्रचार था । उस समय के सभी आर्ष ग्रन्थ संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध होते हैं | महाभारत के पश्चात् सत्य वेदार्थ का लोप और संस्कृत का अति ह्रास हुआ। विद्वानों ने अल्प विद्या और स्वार्थ के वशीभूत होकर जनता को भ्रम में डाला एवं मतवादियों ने बहुत से आर्ष ग्रन्थ नष्ट करके ऋषि - मुनियों के नाम पर मिथ्या ग्रन्थ बनाये | उन के ग्रन्थों में प्रक्षेप किया जिस से सत्यविज्ञान का लोप हुआ । उस नष्ट हुए विज्ञान को महर्षि ने इस ग्रन्थ में प्रकट किया है । महर्षि ने इस ग्रन्थ में बहुमूल्य मोतियों को चुन-चुनकर आर्यभाषा में अभूतपूर्व माला तैयार की, जिस से सर्वसाधारण शास्त्रीय सत्य मान्यताओं को जानकर स्वार्थी विद्वानों के चंगुल से बच सकें ।
- महर्षि दयानन्द कृत ग्रन्थों में सत्यार्थप्रकाश प्रधान ग्रन्थ है | इसमें उनके सभी ग्रन्थों का सारांश आ जाता है ।
- इसके पढ़े बिना कोई भी आर्य ऋषि के मन्तव्यों और उनके कार्यक्रमों को भली प्रकार नहीं समझ सकता एवम् अन्यों के उपदेशों में प्रतिपादित मिथ्या सिद्धान्तों को नहीं पहचान सकता । जिसे अनेक भ्रान्त धारणाएं मस्तिष्क में बैठ जाती हैं जिनके निराकरण के लिए इस ग्रन्थ का अनेक बार अध्ययन सर्वथा अनिवार्य है ।
- इस में आर्यावर्त के मत-मतान्तरों के अन्तर को अनेक स्थानों पर एवम् एकादश समुल्लास में विशेष रूप से खुलकर समझाया गया है
- द्वादश समुल्लास में नास्तिक और बौद्ध,जैन तथा त्रयोदश समुल्लास में ईसाई मत और चतुर्दश समुल्लास में मुस्लिम मतकी समीक्षा की गई है।
- सत्यार्थप्रकाश को पढ़ने से मन में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत होती है और देश के लिए मर-मिटने के लिए व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है। इसमें हमारे देश के गौरव के बारे में बतलाया गया है । इसे पढ़ने से क्रान्तिकारी विचार उत्पन्न होते हैं और देश के लिए कुछ करने के विचार आते हैं । इसे पढ़ने वाला व्यक्ति अपने देश, संस्कृति से प्रेम करने लगता है।
- इस पुस्तक से निम्नलिखित क्रान्तिकारियों को राष्ट्र के लिए मर मिटने की प्रेरणा मिली -
- रामप्रसाद बिस्मिल
- शहीद भगत सिंह
- चन्द्रशेखर आजाद
- लाला लाजपत राय
- वीर सावरकर
- स्वामी श्रद्धानन्द
- श्याम जी कृष्ण वर्मा
- भाई परमानन्द
- पंडित गुरूदत्त
- महात्मा हंसराज आदि |
- इन क्रान्तिकारियों, राष्ट्रभक्तों की जीवनी, आत्मकथा में उन्होंने स्वयं यह लिखा है कि सत्यार्थप्रकाश ने उनके जीवन का तख्ता पलट दिया और उन्होंने स्वयं यह लिखा है कि वे सत्यार्थप्रकाश से प्रेरित रहे हैं।
- सत्यार्थप्रकाश को पढ़ने वाला व्यक्ति सत्य को जान जाता है, वह सभी तरह के पाखण्डों, अंधविश्वासों, कुरीतियों, मिथ्या बातों को जान जाता है और उस व्यक्ति को कभी भूत-प्रेत नहीं सताते, कभी किसी ग्रह का योग उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। जो इस ग्रन्थ को पढ़ लेता है, वह समस्त पाखण्डों, अंधविश्वासों और मिथ्या बातों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है।
- सत्यार्थप्रकाश में वैदिक जीवन पद्धति की सारी विशेषताओं का वर्णन किया गया है।
- सत्यार्थप्रकाश को पढ़ने वाला व्यक्ति ईश्वर का सच्चा स्वरूप जान जाता है ।
- ईश्वर क्या है ? ईश्वर के क्या-क्या कार्य हैं ? ईश्वर कैसे इस जगत का पालन करता है? इस ग्रन्थ में वेदों और अनेक वैदिक ग्रन्थों से प्रमाण दिये गये हैं।
........ वैदिक विचार |
सत्यार्थप्रकाश लिखने के प्रयोजन
ऋषि दयानन्द ने “सत्यार्थप्रकाश” को तीन प्रयोजनों से लिखा था ।- (१) वैदिक धर्म के प्राचीन मन्तव्यों का प्रचार । (२) वर्तमान समय के हिन्दुओं में जो नई-नई कुरीतियां, दोष आ गये थे तथा जिनके कारण वैदिक धर्म में विकार से अनेक मत मतान्तर हो गये थे, उनको दूर किया जाये । ( ३) उन परकीय सम्प्रदाय व सभ्यताओं का सामना किया जाये, जिन्होनें वैदिक आर्य सभ्यता संस्कृति पर आक्रमण करके भारत में अपना प्रभुत्व जमा रखा है । इस आक्रमण का सामना करते हुए विजय पाना व आक्रांन्ता को पराभूत करना इसका उद्देश्य है । यदि इन तीनों बातों को ध्यान में रखकर "सत्यार्थप्रकाश" का अध्ययन किया जाये, तो "सत्यार्थप्रकाश" से बढ़कर इन तीन रोगों की और कोई औषधि नहीं है । वैदिक धर्म प्रेमियों को स्वीकार करना पडे़गा कि वैदिक धर्म की जो रूपरेखा स्वामी दयानन्द ने हमारे सम्मुख रखी है, उससे उत्तम और इतने विस्तार से आज तक के किसी भी अन्य ग्रन्थ में नहीं पायी जाती है । हिन्दू धर्म के वर्तमान रोगों तथा उनकी औषधि जिस उत्तमता से ऋषि दयानन्द ने इस ग्रन्थ में बतलायी है, वह किसी अन्य ग्रन्थ में नहीं मिल सकती है । हिन्दुओं के विभिन्न सम्प्रदायों द्वारा ऋषि दयानन्द का अब तक जो विरोध होता रहा है, वह मात्र उन लोगों के द्वारा ही हुआ है, जिनका जीवन ही सम्प्रदायवाद पर निर्भर करता है । जिन लोगों ने स्वयं को सम्प्रदायवाद के दोष से ऊपर उठा लिया उनको सत्यार्थप्रकाश में कोई दोष दिखाई नहीं देता है ।
अब रही परकीय मतों द्वारा सत्यार्थप्रकाश के विरोध की बात, तो इसका कारण यह है कि यह ग्रन्थ उनके आक्रमण में बाधक बनता है । आर्यसमाज ने इन आक्रमणों का फिर से सामना किया । ये लोग चाहते हैं कि वे निरन्तर आक्रमण करते रहें तथा लोग चुपचाप कोई प्रतिकार किये बिना सिर झुकाते रहें । आर्यसमाज ऐसा करने के लिए कतई तैयार नहीं ।
- “सत्यार्थप्रकाश” की रक्षा के आन्दोलन के समय लिखा गया पं. गंगाप्रसाद उपाध्याय जी के लेख से साभार।
..... पुनर्प्रस्तुति: राजेश आर्य, गुजरात |
सत्यार्थ प्रकाश नवनीत
- १
- जैसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत निवृत्त हो जाता है, वैसे ही परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से सब दोष, दुःख छूटकर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के सदृश जीवात्मा के गुण कर्म स्वभाव पवित्र हो जाते हैं ।(सत्यार्थप्रकाश समुल्लास ७)
- २
- जो परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना नहीं करता है, वह कृतघ्न और महामूर्ख भी होता है, क्योंकि जिस परमात्मा ने इस जगत् के सब पदार्थ सुख के लिए दे रखे हैं, उसके गुण भूल जाना और ईश्वर को न मानना कृतघ्नता और मूर्खता है। (सत्यार्थप्रकाश समुल्लास ७)
- ३
- जैसे कोई अनन्त आकाश को कहे कि गर्भ में आया या मूठी में धर लिया, ऐसा कहना कभी सच नहीं हो सकता है, क्योंकि आकाश अनन्त और सब में व्याप्त है । इससे न आकाश बाहर आता और न भीतर जाता है | वैसे ही अनन्तर सर्वव्यापक परमात्मा के होने से उसका आना कभी नहीं सिद्ध हो सकता है । (सत्यार्थप्रकाश समुल्लास ७)
- ४
- जो मनुष्य जिस बात की प्रार्थना करता है, उसको वैसा ही वर्तमान करना चाहिए, अर्थात् जैसे सर्वोत्तम बुद्धि की प्राप्ति के लिए परमेश्वर की प्रार्थना करे, तो उसके लिए जितना स्वयं से प्रयत्न हो सके उतना किया करे । अर्थात् अपने पुरुषार्थ के उपरान्त प्रार्थना करनी योग्य है ।(सत्यार्थप्रकाश समुल्लास ७)
- ५
- दिन और रात्रि के सन्धि में अर्थात् सूर्योदय और अस्त समय में परमेश्वर का ध्यान और अग्निहोत्र अवश्य करना चाहिए (सत्यार्थप्रकाश समुल्लास ४)
- ६
- जब तक इस होम का प्रचार रहा तब तक आर्य्यावर्त्त देश रोगों से रहित और सुखों से पूरित था | अब भी यज्ञ का प्रचार हो तो वैसा ही हो जायेगा । (सत्यार्थप्रकाश समुल्लास ७)
- ७
- इस प्रत्यक्ष सृष्टि में रचना विशेष आदि ज्ञानादि गुणों के प्रत्यक्ष होने से परमेश्वर का भी प्रत्यक्ष है । (सत्यार्थप्रकाश समुल्लास ७)
- ८
- 'जो इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख और ज्ञानादि गुणयुक्त अल्पज्ञ नित्य है, उसी को "जीव" मानता हूँ ।' (सत्यार्थ प्रकाश - स्वमन्तव्य)
- ९
- क्या पाषाणादि मूर्तिपूजा से परमेश्वर को ध्यान में कभी लाया जा सकता है ? नहीं, नहीं, मूर्तिपूजा सीढ़ी नहीं, किन्तु एक बड़ी खाई है, जिसमें गिर कर वह चकनाचूर हो जाता है । (सत्यार्थप्रकाश समुल्लास ११)
- १०
- जैसे "शक्कर-शक्कर" कहने से मुख मीठा नहीं होता, वैसे ही सत्यभाषणादि कर्म किये बिना और मात्र "राम-राम" कहने से कुछ भी नहीं होगा ।(सत्यार्थप्रकाश समुल्लास ११)
सत्यार्थ प्रकाश में जाटजी और पोपजी की कहानी
यह कहानी यहाँ पढ़ें - जाटजी और पोपजी की कहानी
महर्षि दयानन्द सरस्वती पर भजन
रचनाकार : महाशय धर्मपाल सिंह भालोठिया, भजन-89, मेरा अनुभव (संशोधित) - 2017
तर्ज :- तूने अजब बनाया भगवान, खिलौना माटी का..........
जागे भारत के भाग, दयानन्द आया हे।।
- विरजानन्द से ज्ञान लिया, देश को जीवन दान दिया।
- सांसारिक सुख त्याग, दयानन्द आया हे ।। 1 ।।
- नहीं चेली नहीं चेला था, स्वामी बेधड़क अकेला था।
- खेला था धर्म का फाग, दयानन्द आया हे ।। 2 ।।
- अज्ञान की आँधी आई थी, रात अंधेरी छाई थी।
- दिया ज्ञान का जला चिराग, दयानन्द आया हे ।। 3 ।।
- जुल्म रात-दिन होवें थे, जो तान के चद्दर सोवें थे।
- जगा दिए काले नाग, दयानन्द आया हे ।। 4 ।।
- जहाँ पाखंडियों का डेरा था, वहाँ जाकर उनको घेरा था।
- काशी मथुरा प्रयाग, दयानन्द आया हे ।। 5 ।।
- हजारों विधवा रोवें थी, रो-रो के जिन्दगी खोवें थी।
- उनको दिया सुहाग, दयानन्द आया हे ।। 6 ।।
- वेद का बजा दिया डंका, पाखण्ड की फूँक दई लंका।
- लगा दी उसके आग, दयानन्द आया हे ।। 7 ।।
- सत्य का मार्ग दिखा दिया, भालोठिया को बता गया।
- गाओ धर्म के राग, दयानन्द आया हे ।। 8 ।।
महर्षि दयानन्द की २००वीं जयन्ती
ऋषि जयन्ती पर विवाद क्यों?
सम्मान के योग्य मेरे आर्य विद्वानों एवं आर्य महानुभावो!
बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि जहाँ एक ओर सार्वदोशिक आर्य प्रतिनिधि सभा एवं भारत सरकार के सहयोग से महर्षि दयानन्द की २००वीं जयन्ती, आर्य समाज स्थापना की सार्ध शताब्दी एवं स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान की शताब्दी के संयुक्त कार्यक्रमों की त्रिवार्षिक कार्यक्रम श्रृंखला का आयोजन बड़ी धूमधाम से कर रही है। इसके लिए ज्ञान ज्योति महोत्सव समिति का गठन भी हुआ है, उधर दूसरी ओर आचार्य लोकेश जी दार्शनेय यह अभियान पूर्ण पुरुषार्थ के साथ चला रहे हैं कि ऋषि दयानन्द के जन्म को २०० वर्ष अगले वर्ष अर्थात् वि० सं० २०८१ सन् २०२५ में होंगे। उनके अनुसार ऋषि का जन्म २० सितम्बर १८२५ को हुआ था। मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि आज आर्य विद्वानों को परस्पर झगड़ने, नये-नये विवाद खड़े करने, स्वयं को ही स्वतः प्रमाण मानने तथा विधर्मियों के आक्षेपों के समक्ष गाँधी के बन्दर बन जाने का रोग कहाँ से लग गया है? कुछ समय पूर्व श्री आदित्य मुनि जी एवं डॉ. ज्वलन्त कुमार जी शास्त्री के मध्य ऋषि उद्यान, अजमेर में एक संवाद वा शास्त्रार्थ भी हुआ था‚ उसका परिणाम तो क्या रहा, जानकारी में नहीं आया, परन्तु उसे परोपकारी पत्रिका में अक्षरश: प्रकाशित किया गया था। मैंने भी उसे पढ़ा था। मुझे प्रतीत हुआ कि डॉ. ज्वलन्त कुमार जी शास्त्री का पक्ष कुछ प्रबल था। श्री आदित्य मुनि जी और इनके गुरु पं० उपेन्द्र राव जी के कारनामों से मैं भलीभाँति परिचित हूँ। ये दोनों ही शास्त्रज्ञान से शून्य, परन्तु क्लर्क के कार्य में पूर्ण निपुण रहे हैं। कौन सा वेद मन्त्र कहाँ कितनी बार आया, इसकी तालिका बना कर ही वेद के मर्मज्ञ प्रसिद्ध हो गये। इनके अनुसार वेद पौरुषेय है, उसके कोई नियम नहीं है, उसके उपदेश जंगली हैं.....आदि-आदि। अब ऐसे व्यक्ति भी शोधनिपुण वैदिक विद्वान् के रूप में आर्यों को मान्य हैं, तब तो उन्हें समझाना ही व्यर्थ है।
श्री आचार्य लोकेश जी दार्शनेय की कुछ मान्यताएँ यथा-मास का प्रारम्भ शुक्ल पक्ष से होता है, तो सत्य है, जिसे सम्पूर्ण भारतवर्ष के ज्योर्तिविदों को मानकर कालदर्शकों की एकरूपता बनाने में सहयोग करना चाहिए, परन्तु सृष्टि संवत्, जिसका उल्लेख ऋषि दयानन्द के ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में किया है, को नकारना मुझे तो अभी स्वीकार नहीं हैं। इस विषय में रामलाल कपूर ट्रस्ट एवं आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट में मतभेद रहे हैं। रामलाल कपूर ट्रस्ट के विद्वान् संधिकाल जोड़कर १९७ करोड़ वर्ष वाला सृष्टि संवत् मानते रहे हैं और आ. सा. प्रचार ट्रस्ट के विद्वान् ऋ०भा० भू० वाला १९६ करोड़ वाला संवत् मानते रहे हैं। ‘दयानन्द सन्देश’ का इस विषय में सृष्टिसंवत् विशेषांक भी बहुत वर्ष पूर्व प्रकाशित किया था और तभी मैंने उसे पढ़ा था। इसमें मुझे आचार्य श्री राजवीर जी शास्त्री का ही १९६ करोड़ वर्ष वाला पक्ष अधिक तर्कसंगत प्रतीत हुआ। दु:ख की बात यह है कि आर्यसमाज में आज भी दोनों पक्ष चल रहे हैं।
आचार्य लोकेश जी दार्शनेय हमारे एक न्यासी प्रो० (डॉ०) वसन्त कुमार जी मदनसुरे, अकोला (महाराष्ट्र) द्वारा उनके पक्ष पर उठायी गयी किसी भी आपत्ति का कभी उत्तर नहीं देते। प्रो० वसन्त जी सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि उनका वैदिक ग्रन्थों का गम्भीर स्वाध्याय है और इंजीनियरिंग के प्रोफेसर होने से उनकी तर्क व विश्लेषण की क्षमता अच्छी है। इस कारण आचार्य दार्शनेय जी को उनसे संवाद करना चाहिए। मैं यहाँ २०० वर्ष वाले बिन्दु पर यह कहना चाहता हूँ कि निश्चित ही महर्षि के जन्म को २०८१ वि० सं० में ही दो सौ वर्ष पूर्ण होंगे, परन्तु टंकारा के कार्यक्रम के मंच का चित्र प्रिय डॉ. मोक्षराज आर्य ने मुझे भेजा था। उस पर २००वाँ जन्मोत्सव लिखा था, न कि २००वीं जयन्ती। १९९ वर्ष पूर्ण होने पर २००वाँ जन्म दिवस तो हो ही जाता है, क्योंकि प्रथम जन्मोत्सव तो १८८१ में ही उनके जन्म के समय मनाया होगा। तब २०८० में २००वाँ जन्मोत्सव क्यों नहीं होगा? हाँ, जन्म की २००वीं वर्षगाँठ नहींं होगी, वह १९९ वीं ही होगी। बैनरों पर २००वीं जयन्ती लिखने का तात्पर्य तो यही है कि २०० वर्ष के आगे व पीछे के कुल तीन वर्ष तक कार्यक्रम मनाने हैं। इस शृंखला का नाम २००वीं जयन्ती है, इसके अतिरिक्त शृंखला का नाम और क्या रखा जा सकता था? मैं यह स्पष्ट कर दूँ कि मैं न तो सार्वदेशिक सभा और ज्ञान ज्योति महोत्सव समिति का अधिवक्ता वा प्रवक्ता हूँ और न इनका कोई साधारण सा सदस्य ही हूँ, पुनरपि प्रत्येक अच्छे कार्य का समर्थन करना मेरा धर्म है, क्योंकि ऋषि दयानन्द मेरे भी तो आदर्श हैं।
मैं तो सभी विद्वानों से यही चाहूँगा कि वेदादि शास्त्रों पर जो घृणित आक्षेप विधर्मियों ने किए हैं वा कर रहे हैं, उनके लिए अपने बौद्धिक व शास्त्रीय बल का प्रयोग करें, न कि परस्पर विवाद खड़ा करके रहे-सहे संगठन को और भी खण्ड-खण्ड करें। हाँ, १२ फरवरी को जन्म दिन मनाना बौद्धिक दासता का प्रतीक है, इसे अवश्य दूर करके जब अगले वर्ष ऋषि जन्म को २०० वर्ष पूर्ण हो जायें, तब फाल्गुन कृ० दशमी को ही मनाना चाहिए और सरकार को भी यह बात बता देनी चाहिए। कहीं दीपावली, होली, श्रीकृष्णजन्माष्टमी, श्रीरामनवमी को अंग्रेजी तिथियों से मनाने की कभी चाल न चली जाये? यह भारत है, जिसका मात्र शरीर ही बचा है, आत्मा तो कब का निकल कर कहीं चला गया है। मैंने सभी विद्वानों व सभाओं को विधर्मियों द्वारा प्राप्त आक्षेपों के १३४ पृष्ठ भेजे थे, उस पर सब मूक बधिर बने हैं, लेकिन जयन्ती पर अपनों से ही विवाद कर रहे हैं, युद्ध के लिए उद्यत हैं। हाँ‚ इतना मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि ज्योतिष विषय पर आचार्य लोकेश जी‚ स्वामी श्री ब्रह्मानन्द जी सरस्वती‚ कामारेड्डी के साथ अधिकारी विद्वानों का प्रीतिपूर्वक संवाद अवश्य होना चाहिए।
मैं आचार्य लोकेश जी आदि से यह जानना चाहता हूँ कि जब लम्बे समय से फा० कृ० दशमी को ही सम्पूर्ण आर्य जगत् जन्मदिन मनाता रहा है और अब भारत सरकार भी आर्य समाज के इस अभियान में साथ है, तब आप सरकार के साथ-साथ सभी विधर्मियों को आखिर क्या बताना चाहते हैं? आप यह दर्शाना चाहते हैं कि देखो, आर्य समाजियों से बढ़ कर स्वजाति द्रोही और कोई नहीं हो सकता। आपके मनोरथ सिद्ध हो भी जायें, तो उससे लाभ किसको होगा? यदि मान लें कि यह जन्मतिथि मिथ्या भी हो, तो क्या धर्म रसातल को चला जायेगा? वेद व आर्य सनातन धर्म पर विधर्मी आक्रमण कर रहे हैं, आपकी पीढ़ी पाश्चात्य कुसंस्कारों की दासी बन चुकी हैं, ऋषियों व देवों को अपमानित किया जा रहा है, ऋषि दयानन्द के ही नहीं, अपितु सभी आर्ष ग्रन्थों पर घृणित आरोप लगाये जा रहे हैं, उससे आप को कोई पीड़ा नहीं होती। जन्मतिथि बदलने से क्या धर्म बच जायेगा? मानवता बच जायगी?
जरा विचारो! जिस कार्य को करने से धर्म बचे, संगठन बचे, मानवता के प्राण बचें, उस पर कान धरो, अन्यथा आप व सम्पूर्ण संगठन देश में उपहास के पात्र बन कर रह जायेंगे। आप की इसी फूट के कारण ही आर्य समाज की तेजस्विता समाप्त हो चुकी है, कोई पूछता नहीं है। यह बात राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से सीखो। लडना है तो विधर्मियों से बौद्धिक युद्ध करो, अन्यथा मौन रहना ही अच्छा है। मैं मानता हूँ कि जन्मतिथि की यथार्थता की जाँच भी होनी चाहिए, परन्तु इस समय देश व संसार में वेदादि शास्त्रों की दशा, जो मृतप्राय है और सारा देश और स्वयं आर्य समाज भी बौद्धिक दास बन गया है, उसकी रक्षा करना सर्वाेपरि धर्म है। जब इस दशा की चर्चा विद्वानों से करता हूँ, तो वे मुझे ही कोसने लग जाते हैं और जयन्ती मनाने से वेद की रक्षा हो जायेगी, ऐसा मान बैठे हैं। पुनरपि मैं इन समारोहों के लिए सार्वदेशिक सभा एवं सम्पूर्ण आर्यजगत् को बधाई देता हूँ। ईश्वर सबको सद् बुद्धि प्रदान करे।
- –आचार्य अग्व्रित नैष्ठिक
संदर्भ : (19 फरवरी 2024 को एक WhatsApp ग्रुप द्वारा फैलाया गया सन्देश
महर्षि दयानन्द की 200वीं जन्म जयन्ती के कुछ चित्र
Jatland links (online books of Swami Dayanand)
- व्यवहारभानु (महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा रचित लघुग्रंथ) - Read online at Jatland wiki
- गोकरुणानिधि (महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा रचित लघुग्रंथ) - Read online at Jatland wiki
- आर्य्योद्देश्यरत्नमाला (महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा रचित लघुग्रंथ) - Read online at Jatland wiki
- संस्कृतवाक्यप्रबोध - Read online at Jatland wiki
Also see
References
- ↑ Jat History Dalip Singh Ahlawat/Chapter VII (Page 603-605)
External Links
Back to The Reformers



